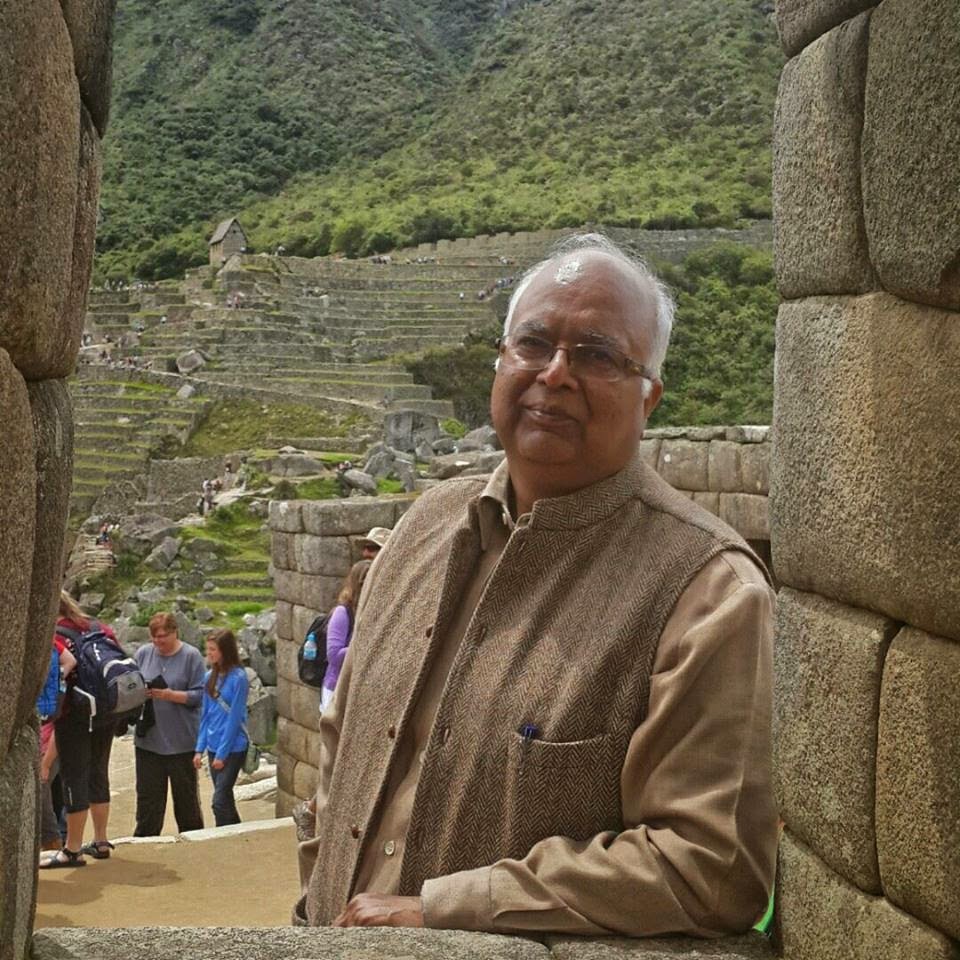जनसत्ता के संपादक और लेखक ओम थानवी को उनकी यात्रा-विचार पुस्तक ‘मुअनजोदड़ो’ के लिए २०१४ के २४ वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा हुई है. क्या है मुअनजोदड़ो ? प्रो. माधव हाड़ा ने इस किताब के माध्यम से भारतीय महाद्वीप के इतिहास और पुरातत्व पर ओम थानवी के नजरिये को देखा - परखा है.
मुअनजोदड़ो : विवादों की गर्द, कल्पना का दलदल और इतिहास की गाड़ी
माधव हाड़ा
किताब के आगे के हिस्से के वृत्तांत में विवेचन और विश्लेषण का पुट आ जाता है. लेखक अब एक शोधार्थी की तरह पहले मुअनजोदड़ो के महत्व पर रोशनी डालता है. उसके अनुसार यहां की खुदाई से रातों-रात भारत के इतिहास का नक्शा बदल गया.(पृ.38) यही बात बहुत पहले रोमिला थापरने भी कही थी. उनके अनुसार इस खोज से पारंपरिक भारतीय इतिहास का प्रारंभिक भाग पौराणिक कहानी बनकर रह गया. लेखक के अनुसार “सौ साल पहले भारत का दुनिया में महज दावा था कि उसकी सभ्यता प्राचीन है लेकिन सिंधु घाटी के हड़प्पा और मुअनजोदड़ो की खुदाई ने इस दावे को हकीकत में बदल दिया.”(पृ38.) उसके अनुसार सिंध के मुअनजोदड़ो, पाक-पंजाब के हड़प्पा, राजस्थान के काल ीबंगा और गुजरात के लोथल व धौलावीरा की खुदाई में हासिल पुरावशेषों ने यह अच्छी तरह साबित कर दिया कि सिंधु घाटी समृद्ध और व्यवस्थित नागर संस्कृति थी. उसके निवासी उन्नत खेती और दूर-दूर तक व्यवसाय करते थे. वे उपकरणों का इस्तेमाल करते थे, शुद्ध नाप-तौल जानते थे और उनका रहन-सहन और नगर नियोजन उन्नत किस्म का था. लेखक को इस सभ्यता की जो बात सबसे महत्वपूर्ण लगती है वो यह कि इसमें साक्षरता, सुरुचि और संपन्नता थी. इस सभ्यता के सौंदर्यबोध से भी वह अभिभूत है. वह इसके लिए यहां मिली बहुचर्चित याजक नरेश और कांसे से निर्मित निर्वसन नर्तकी युवती का विस्तृत वर्णन करता है. लेखक यहीं मोएनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो आदि प्रचलित नामों के स्थान पर इस स्थान के असल नाम मुअनजोदड़ो का भाषायी अर्थ भी स्पष्ट करता है. वह लिखता है, “मुआ यानि मृत.. बहुवचन में मुअन, मुआ का सिंधी प्रयोग है. दड़ा माने टीला. मुअन-जो-दड़ो: मुर्दो का टीला.” (पृ.44) मुअनजोदड़ो का महत्व स्थापित कर देने के बाद लेखक इस स्थान की खोज और इसमें लगे लोगों की मेहनत का सिलसिलेवार ब्योरा देता है. 1924 ई. में सामने आए मुअनजोदड़ो की खोज का श्रेय आम तौर परकाम भारतीय पुरातत्त्ववेत्ताओं ने ही किया. हड़प्पा मेंयह काम हीरानंद शास्त्रीने 1909ई. में, जबकि मुअनजोदड़ो में यह काम राखालदास बंद्योपाध्यायने 1922-23 ई. में किया. मुअनजोदड़ो में बंद्योपाघ्याय के बाद माधोस्वरुप वत्स और काशीनाथ दीक्षितने भी खुदाई करवाई.
कर ाची से मुअनजोदड़ों तक की यात्रा का वृत्तांत और इस बहाने मुअनजोदड़ों और सिंधु सभ्यता की यह मीमांसा कई मायनों में खास है. यह हमारे ज्ञान और समझ को पुर्ननवा करती है और उसमें बहुत कुछ नया भी जोड़ ती है. वृत्तांत के आरंभ में लेखक ने हवा में उडने और जमीन पर चलने में फर्क होने की जो बात कही है, वह अंत तक उसके जेहन में रही है. उसने आद्यंत हवा में उडने के बजाय अपने पांव पुरातात्त्विक तथ्यों की जमीन पर मजबूती से टिकाए रखे हैं. साहित्यिक संस्कारों के बावजूद उसने अपने कल्पना के घोड़ों को दौडने नहीं दिया है. मुअनजोदड़ो और सिंधु सभ्यता संबंधी अपने विवेचन-विश्लेषण में वह उन सब मत-मतांतरों और संभावन ाओं का ब्योरा देता है, जो अब तक सामने आए हैं. खास बात यह है कि वह न तो झटके से किसी खारिज करता है और न ही जल्दबाजी में कुछ स्वीकार करता है. इस संबंध में पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों के बीच जो मामले अभी अनिर्णीत हैं, वह उनका केवल ब्योरा देकर आगे बढ़ जाता है.
इस सभ्यता की लिपि और रुपांतरण को लेकरउसका रवैया ऐसा ही है. अपनी तरफ से कोई टिप्पणी करने में उसने बहुत संयम बरता है. जहां उसने टिप्पणी की है वहां उसका नजर ियाएक दमपर्यवेक्षण और अनुभव के साक्ष्य दिए है. सिंधु सभ्यता और उसके बाद विकसित वैदिक संस्कृति की सांस्कृतिक संरचना अलग-अलग है, लेकिन भारतीय जीवन दृष्टि में सिंधु सभ्यता की निरंतर ताआधार ित हैं. शांति, अहं का विलय, कला के लघु रूप और प्रकृति सानिध्य, सिंधु सभ्यता की ये कुछ बातें भारतीय जीवन दृष्टि में लेखक अनुसार आज भी है. लेखक इसके कुछ और मुखर और प्रत्यक्ष साक्ष्य भी देता है. वह कहता है कि “हम आज भी ईंटें उसी आकार में और वैसे ही सेंक कर बरतते है जैसे 5हजार साल पहले बरती गई थी. खेत, हल, सिंचाई, फसलें, बैलगाडियां, गहने, घर, कुएं, जलनिकास , कला व शिल्प की अनेक परंपराए आज भी वैसी ही चली आती हैं, जैसी तब थीं. मुअनजोदड़ो की ‘नर्तकी’ के बाएं हाथ मेंकलाई से कंधे तक जो ‘चूड़ा’ है वह भारत और पाकिस्तान के थार में औरतों के हाथों पर आज भी इसी रूप में देखा जा सकता है.”(पृ.112) इन अंतर्सूत्रों को आधार बनाक र यह निष्कर्ष निकाल ना आसान है कि यह सभ्यता खत्म नहीं हुई, इसका रुपांतरण हुआ, लेकिन लेखक ऐसी कोई टिप्पणी करने से भी बचता है. नवीन तम अन्वेषण भी यही कहते है कि सिंधु नदी के बहाव में बदलाव के कारण लोग इस कृषि प्रधान सभ्यता के नगरों को छोडकर भोजन की तलाश यहां-वहां बिखर गए होंगे और उन्होंने ‘कुछ छोडकर और कुछ जोडकर’ जीवन का सिलसिला जारी रखा होगा. लेखक ने एक जगह लिखा भी है कि “संस्कृतियां इसी तरह कुछ छोड़ते और जोड़ते हुए आगे बढ़ती है.“ (पृ.112)
वृत्तांत का गद्य शानदार है. विवेचन-विश्लेषण और विचार के लिए हिंदी में इस्तेमाल किए जानेवाले भारी भरकम और जलेबीदार वाक्यों वाले गद्य से एकदम अलग, यह छोटे-छोटे वाक्यों वाला, बोलचाल की नाटकीयता से भरपूर बहता हुआ गद्य है. कुछ अटपटे शब्द प्रयोग, जैसे अनुकूलित वायु, अवजलनिकास ी आदि चुभते हैं. ये इस किताब की भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं. धर्मेन्द्र पारे के रेखाचित्र वृत्तांत को पढने-समझने बहुत मदद करते हैं, अलबत्ता इनके शीर्षक नहीं होने से कई बार मुश्किल जरूर होती है. पाठक को रुक कर इनके संबंध में कयास लगाना पड़ता है.
![]() _____________________
_____________________
प्रो.माधव हाड़ा
अभी कुछ समय पहले तक हिंदी के साहित्यिक विमर्श का दायरा केवल अपने तक सीमित था. साहित्य में साहित्येतर अनुशासनों की मौजूदगी घुसपैठ की तरह अवांछनीय थी. समाज विज्ञान, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, संगीत आदि अनुशासनों के साथ संवाद और अंतर्क्रिया को इसमें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था. अब हालात बदल रहे हैं. हिंदी के साहित्यिकों की समझ अब साहित्य की सीमा लांघ कर ज्ञान के साहित्येतर अनुशासनों तक पहुंच गई है. अब वे ज्ञान के दूसरे अनुशासनों की समझ के साथ साहित्य में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे साहित्य की दुनिया पहले की तुलना में अधिक समृद्ध ओर बड़ी हुई है. मुअनजोदड़ो विख्यात पत्रकार ओम थानवीकी पहली किताब है. यह एक यात्रा वृत्तांत है जो इतिहास, संस्कृति और पुरातत्त्व की गहरी समझ के साथ लिखा गया है. खास बात यह है कि मुअनजोदड़ो को यह किताब ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक के साथ सांस्कृतिक दिलचस्पी के केन्द्र में लाती है.
मुअनजोदड़ो की खोज से पारंपरिक भारतीय इतिहास का नक्शा बदल गया था. इतिहासकारों और पुरातत्त्ववेत्ताओं को इस खोज से अपनी धारणाओं में कई उलट-फेर करने पड़े. अब तक सर्वाधिक प्राचीन मानी जाने वाली वैदिक संस्कृति के साथ इसका तालमेल मुश्किल हो गया. किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि सुमेरी सभ्यता के समकक्ष यह समृद्ध सभ्यता खत्म कैसे हो गई. इसकी लिपि अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया. इतिहासकार और पुरातत्त्ववेत्ता इस संबंध में केवल कयास लगाते रहे, जिससे विवादों की झड़ी लग गई. लेखक के शब्दों में कहें तो “सिंधु घाटी की सभ्यता को लेकर खुदाई कम हुई है, विवादों की जड़ें ज्यादा खोदी गई हैं.”(पृ.109) हिंदी के साहित्यिक भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने मुअनजोदडो के इतिहास की गाड़ी को कल्पना के दलदल में घसीट लिया. लेखक ने इस वृत्तांत में इन विवादों और कल्पना के दलदल की विस्तार से पड़ताल की है. उसने उन पुनरुत्थानवादी प्रयासों को खारिज किया है, जो इस सभ्यता हिंदू सभ्यता साबित करना चाहते हैं. उसने पूरी तरह देशज इस सभ्यता की वर्तमान में निरंतरता के कुछ व्यावहारिक सूत्रों की भी खोज की है.
यह किताब शुरू यात्रा वृत्तांत से और खत्म पुरातात्त्विक विवेचन-विश्लेषण से होती है. किताब के शुरुआती पृष्ठों में कराची से मुअनजोदड़ो तक का यात्रा वृत्तांत है. यहां लेखक पाठकों के सिंध संबंधी ज्ञान और समझ को कभी पुनर्नवता तो कभी समृद्ध करता चलता है. वह स्थानीय सिंधी सहयात्री के सहयोग से सिंध को उसके अतीत और वर्तमान की जड़ों में जाकर समझने की कोशिश करता है. वह देखता है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम राज सबसे पहले सिंध में काय म हुआ, मगर हिंदू-मुस्लिम फसाद वहां कभी नहीं हुए. वह इसके कारण ों की तह में जाता है और पाता है एक तो सदियों पहले यहां कायम बौद्ध मत के सहनशीलता और करुणा की गहरी जड़े छोड़ जाने से और दूसरे सूफियों के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ. (पृ.23) बंटवारे और आजादी के बाद सिंध में बड़े पैमान पर हुए जातीय दंगों के कारणों की पड़ताल करते हुए वह इस निष्कर्ष पहुंचता है कि यह सिंध में सिंधियों के हाशिए पर चले जाने कारण हुए. बंटवारे के बाद सबसे अधिक मुहाजिर उत्तर प्रदेश और पाक पंजाब से यहां आए, सिंधी आबादी यहां केवल आठ प्रतिशत रह गई और सिंधी भाषा की जगह उर्दू और अंग्रेजी ने ले ली. सिंध के लोगों ने इसे अपनी पहचान पर हमला समझा. “जातीय अस्मिता की इस कशमकश में सिंध में ‘सिंधु देश’ के लिए ‘जिए सिंध’ आंदोलन उठ खड़ा हुआ.” (पृ.25 ) कराची से मुअनजोदड़ो तक की इस बस यात्रा के दौरान आने वाले दो शहरों के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व से भी लेखक रूबरू करवाता है. उसकी इस यात्रा का पहला पड़ाव है सेवण. रुना लैला, आबिदा परवीन, नुसरत फतह अलीखान और न जाने कितने और गायकों के मुंह से इस शहर का नाम सुना है, लेकिन इसके महत्व पर रोशनी अब लेखक डालता है. वह बताता है कि सेवण सूफी फकीर शाहबाज कलंदर का स्थान है, जिन्हें मुस्लिम पीर और हिंदू भर्तृहरि का अवतार मानते हैं.(पृ.31) लरकाणा, जिसे लेखक अपने स्थानीय सहयात्री के आग्रह पर सही लाड़काणा कहता है, के आते ही लेखक उसकी पहचान जुल्फीकार अली भुट्टो के शहर के रूप में करता है. बाद वह इसे सूफी गायिका आबिदा परवीन और फिल्मकार कुमार शाहनी के शहर के रूप में भी याद करता है.(पृ.34)
मुअनजोदड़ो का मुआयना लेखक ने बहुत बारीकी और विस्तार से किया है. यह एक पुरातत्ववेत्ता और इतिहास कारभी है. वह कहता है कि “मुअनजोदड़ो की खूबी यह है कि इस आदि मशहर की सडककों और गलियों में आप आज भी घूम-फिर सकते हैं. यहां का सभ्यता और संस्कृति का सामान चाहे अजायबघरों की शोभा बढ़ा रहा हो, शहर जहां था अब भी वहीं है. आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिका कर सुस्ता सकते हैं. वह कोई खंडहर क्यों न हो, किसी घर की देहरी पर पांव रखकर सहसा सहम जा सकते हैं, जैसे भीतर कोई अब भी रहता है.“ (पृ.50) मुअनजोदड़ो की इमारतों, सड़कों का आदि का विवरण इस किताब में इस तरह है कि आपको यह जीवंत नगर की तरह लगता है. यह विवरण इतिहास और पुरातत्त्व की किताबों में भी है, लेकिन यहां एक कृतिकार की आंख से देखा गया विवरण है. उसके अनुसार सिंधु नदी के दाहिने तट पर पांच किलोमीटर के विस्तार में फैला हुआ यह 2600ई.पू का यह नगर दो भागों में बंटा हुआ है. दुर्ग टीले के पश्चिमी भाग में स्थित सार्वजनिक महत्व के भवनों का इलाका गढ़ कहलाता है, जिसमें सभा भवन, ज्ञानशाला, अन्नागार और स्नानागार हैं. दुर्ग टीले के सामने आबादी वाला शहर है. नगर नियोजन की यह पद्धति बाद में भी दिखाई पड़ती है. लेखक का मानना है कि यह रास्ता दुनिया को मुअनजोदड़ो ने दिखाया लगता है.(पृ.53) लेखक इन सभी इमारतों और बस्तियों का जायजा लेता है.
अपने मूल स्वरूप के बहुतनजदीक तक बचे हुए स्नानागार की पड़ताल लेखक ने अपेक्षाकृत विस्तार से की है. उसके अनुसार यह सिद्ध वास्तुकला का उदाहरण है.(पृ.55)मुअनजोदडो का नगर नियोजन और अवजल निकासी प्रबंध खास तौर पर लेखक का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. मुअनजोदड़ो के आबादी वाले इलाके का कोई घर सड़क पर नहीं खुलता. उनके दरवाजे अंदर गलियों में है. लेखक कहता है कि नगर नियोजन यही शैली आधुनिक शहर चंडीगढ़ में ली कार्बूजिए ने इस्तेमाल की है.(पृ.61)मुअनजोदड़ो के घरों से गंदे पानी की निकासी के लिए बनी होदियों और नालियों के जाल पर लेखक अमर्त्य सेनके शब्द उधर लेकर कहता है कि “मुअनजोदड़ो के चार हजार साल बाद तक अवजल निकासी की ऐसी व्यवस्था देखने में नहीं आई.”(पृ.63)यहां कुंओं की मौजूदगी के संबंध में वह इरफान हबीबको उद्घृत करता है जो लिखते है कि “सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञान संस्कृति है, जो कुंए खोदकर भूजल तक पहुंची.”(पृ.63) बस्ती में घूमते हुए उसका ध्यान इस ओर जाता है कि एक तो कुओं को छोडकर सब कुछ चौकोर या आयताकार है और दूसरे, कमरे आकार में बहुत छोटे हैं और खिड़कियों और दरवाजों पर छज्जे नहीं है. वह इस संबंध में कयास तो लगाता है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता. मुअनजोदड़ो के संग्रहालय का जायजा लेते हुए लेखक का ध्यान कुछ और बातों पर भी जाता है. एक तो वहां प्रदर्शित चीजों में कोई हथियार नहीं है और दूसरे इन चीजों में प्रभुत्व या दिखावे का तेवर नदारद है. हथियार नहीं होने के संबंध में वह विशेषज्ञों की राय को आधार बनाक र निष्कर्ष निकाल ता है कि वहां अनुशासन शक्ति आधारित नहीं था. दिखावे का तेवर नहीं होने के संबंध में लेखक का मत है कि यह लो-प्रोफाइल सभ्यता थी, जो लघुता में भी महत्ता का अनुभव करती थी.(पृ.75)
अपने मूल स्वरूप के बहुत
मुअनजोदड़ो से जुड़ी उन दो चर्चित गुत्थ्यिों से लेखक भी रूबरू होता है, जिनसे अब तक सभी पुरातत्त्ववेत्ता और इतिहासकार रूबरू हो चुके हैं और कोई निष्कर्ष निकालने में असफल रहे हैं.
पहली गुत्थी यह है कि सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हो गई. अत्यधिक भूमि दोहन, भूकंप-बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा, जंगलों का विनाश और व्यापार शैथिल्य जैसे कई संभावित कारणों पर विचार के बाद लेखक ताजा भूगर्भगीय अध्ययनों के हवाला देते हुए संभावना व्यक्त करता है कि इसका विनाश समुद्र का स्तर ऊपर उठने से हुआ होगा. समुद्र का स्तर ऊपर उठने से सिंधु का प्रवाह धीमा हो गया होगा और उसमें खेतों में गाद भर गई होगी, जिससे क्षार बढ़ गया होगा.(पृ.83)
दूसरी ज्यादा पेचीदा गुत्थी यह है कि वैदिक संस्कृति और सिंधु सभ्यता का संबंध किस तरह का है. दरअसल इस सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास का ढांचा इस तरह बदला है कि उसके इस आरंभिक चरण को परवर्ती चरणों से जोडना मुश्किल काम हो गया. पुनरुत्थानवा दी इतिहासकारों और कल्पनाजीवी साहित्यकारों ने कल्पना की घुड़दोड़ से अर्थ का अनर्थ कर दिया है. लेखक इस संबंध में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय यही कहता है कि “अगर देशज-विदेशज की भावुकता के जंजाल में न पड़ें,तो वैदिक संस्कृति और सिंधु सभ्यता, दोनों , भारत के इतिहास की शान है.”(पृ.87)
लेखक सिंधु सभ्यता की तीसरी गुत्थी उसकी अबूझ लिपि को समझने के प्रयासों का ब्यौरा भी देता है, लेकिन इस संबंध में उसका मत है कि “लिपि का रहस्य सिंधु सभ्यता की खोज के पहले जहां था, आज भी वहीं है.” (पृ.89) वृत्तांत के उत्तरार्द्ध में लेखक ने सिंधु घाटी सभ्यता के साहित्य में इस्तेमाल की भी खोज-खबर ली है. उसका कहना है कि “साहित्य के लोगों ने पुरातत्त्व और इतिहास के लोगों की तुलना में इस संबंध में ज्यादा लिखा है लेकिन पुरातत्त्व का लाभ न उठा पाने से हिंदी में सांस्कृतिक इतिहास की चर्चा अप्रामाणिक ही नहीं, कही-कहीं नितांत काल्पनिक हो गई है.”(पृ.93) लेखक ने वासुदेवशरण अग्रवालकी भारतीय कला संबंधी एकाधिक स्थापनाओं को पुरातात्त्विक साक्ष्यों से पुष्ट नहीं होने के कारण गलत माना है. रामविलास शर्माद्वारा किए गए सिंधु सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बेमेल गठजोड़ की भी उसने जमकर खबर ली है. रामविलास शर्मा की यह धारणा कि वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता से प्राचीन थी लेखक के अनुसार बलूचिस्तान की पहाड़ियों में मिले लगभग नौ हजार साल पहले के सिंधु सभ्यता के शुरुआती दौर के प्रमाण मिलने से निराधार हो जाती है.(पृ.97) डी. डी. कोसांबी और राहुल सांकृत्यायनकी आर्य आक्रमणों से सिंधु सभ्यता के विनाश की धारणा को भी लेखक पुरातत्त्व सम्मत नहीं मानता. उसके अनुसार हमले की परिकल्पना प्रत्यक्ष और पारिस्थिति क साक्ष्य से निर्मूल साबित हुई है.(पृ.103) साहित्य में हुए सिंधु सभ्यता के इस्तेमाल के संबंध में अंत में यहीं निष्कर्ष निकलता है कि “इतिहास की गाड़ी को कल्पना के घोड़े लगाकार दलदल में फंसाया जा सकता है.”(पृ.104)
इस सभ्यता की लिपि और रुपांतरण को लेकर
वैदिक संस्कृति से इस सभ्यता की भिन्नता संबंध में पुरातत्त्ववेत्ता और इतिहासकार लगभग एक राय हैं. वैदिक संस्कृति में इस सभ्यता की निरंतरता नहीं होना लेखक को भी विस्मित करता है. लेखक ने अपने पर्यवेक्षण और पुरातत्त्ववेत्ताओं के साक्ष्य से एक संकेत किया है कि यह सभ्यता समाज पोषित थी.(पृ.78) कहीं ऐसा तो नहीं कि वैदिक सभ्यता भी समाज पोषित सभ्यता हो और उपलब्ध साहित्यिक साक्ष्यों की धुंध में उसका यह रूप दब गया हो. यह तो तथ्य है कि वैदिक सभ्यता की अवधारणा के विकास में पुरातात्त्विक साक्ष्यों के साथ साहित्यिक साक्ष्यों की निर्णायक भूमिका है. साहित्यिक साक्ष्यों में कल्पना और आदर्श का पुट आ ही जाता है, यह लेखक ने भी स्वीकार किया है.(पृ.104 ) ब्राह्मण साहित्यिक साक्ष्य दैनंदिन सामाजिक वास्तविकता से कटे हुए थे, यह भी अब सिद्ध हो गया है. वैदिक सभ्यता को साहित्यिक साक्ष्यों से अलग पुरातात्त्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार नए सिरे से देखा-परखा जाए तो शायद उसके समाजपोषित होने के साक्ष्य वहां भी मिले. उपनिवेशकाल से पहले हमारी संस्कृति की जीवंतता में समाजपोषण की सर्वोपरि भूमिका थी, इधर के नए अन्वेषणों का निष्कर्ष भी यही है.
आर्य बाहर से आए थे, यह धारणा हिंदुत्ववादी मंसूबों के अनुकूल नहीं थी, इसलिए हड़प्पा और मुअनजोदड़ो की खोज से वे सक्रिय हो गए. उन्होंने ऋग्वैदिक सभ्यता को खींच- खांचकर हड़प्पा पर लाद दिया. विडंबना यह है कि इस संबंध में हिन्दुत्ववादी, मार्क्सवादी और आर्यसमाजी, सब एक हो गए.(पृ.104) हिंदी में रामविलास शर्माऔर भगवानसिंह के अन्वेषण की दिशा भी कमोबेश यही थी. यह अच्छी बात है कि लेखक ने सजगतापूर्वक अपनी पडताल की दिशा पुनुरुत्थानवादी नहीं होने दी है. उसने बहुत तार्किंग ढंग से इन सभी प्रयासों की निरर्थकता भी सिद्ध की है. हिंदुत्ववादी ताकतों द्वारा सिंधु सभ्यता को सिंधु-सरस्वती सभ्यता नाम देने का भी उसने विरोध किया है. उसके अनुसार सरस्वती वेदों में जरूर है पर उसका भौतिक और ऐतिहासिक पक्ष अभी खोज के दायरे में है.(पृ97.) वैदिक सभ्यता को हड़प्पा से भी पहले स्थापित करने की रामविलास शर्मा को धारणा भी उसके अनुसार बहुत काल्पनिक है.(पृ.96) नए पुरातात्त्विक साक्ष्य उसके अनुसार इस धारणा के एकदम उलट है.
मुअनजोदड़ो के ऐतिहासिक और पुरातात्त्विक महत्व पर तो विश्व भर के विशेषज्ञों को ध्यान गया है, लेकिन लेखक की खूबी यह है कि उसने उसके सांस्कृतिक महत्व पर भी रोशनी डाली है. उसके अनुसार यह भारतीय उपमहाद्वीप की साझा विरासत है.(पृ.113) विभाजन के बाद इसका महत्व और बढ़ गया है. यह अलगाव और मतभेदों के बीच भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सभ्यता के एक होने का सबूत है. लेखक के शब्दों में “हमारी विविधता में यह एक केन्द्रीय सूत्र है.” (पृ.113) लेखक ने इस संबंध में सिंध के एक नेता का बहुत अर्थपूर्ण कथन उद्घृत किया है जो कहता है कि “हम चंद दशकों से पाकिस्तानी हैं, कुछ सदियों से मुसलमान, मगर हजारों साल से सिंधी हैं.” (पृ.113)
 _____________________
_____________________प्रो.माधव हाड़ा
संपर्क: कार्यकारी महिला छात्रावास के पास, पी.डब्ल्यू. डी. क़ॉलोनी,
सिरोही 307001 राजस्थान
फोन +91 2972 220428 मो. +91 94143 25302
e-mail: madhavhada@gmail.com