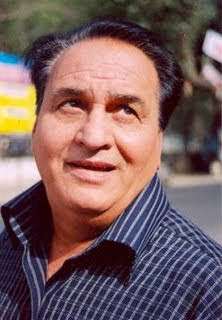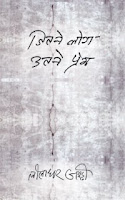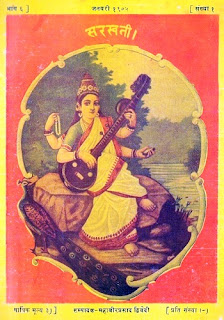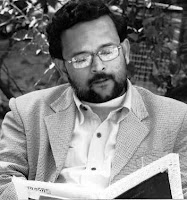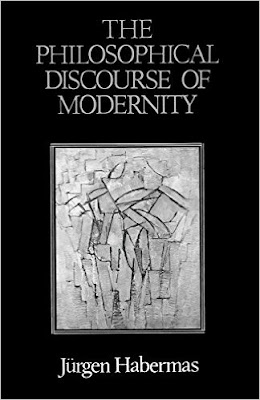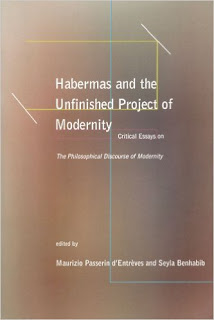विमल चन्द्र पाण्डेय
प्रश्न-मेरे घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और मेरे पिताजी की नौकरी छूट गयी है. वो चाहते हैं कि मैं घर का खर्च चलाने के लिये कुछ काम करूं लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता हूं. मैं अपनी पढ़ाई के साथ-साथ उनकी मदद भी करना चाहता हूं और चाहता हूं कि कोई ऐसा काम कर सकूं कि पढ़ाई भी हो सके और कुछ कमाई भी, मैं क्या करूं ? - मनोज कनौजिया, वाराणसी
उत्तर-आपका पहला फ़र्ज़ है अपने पिताजी की मदद करना लेकिन यह भी सच है कि बिना उचित ज्ञान और डिग्री के कोई अच्छा काम मिलना मुश्किल है. दिक्कत यह भी है कि ऐसा कोई काम कहीं नहीं है जो करके आप पैसे भी कमाएं और साथ में पढ़ाई भी कर सकें. काम चाहे जैसा भी हो, अगर वह आप पैसे कमाने के लिये कर रहे हैं तो वह आपको पूरी तरह चूस लेता है और किसी लायक नहीं छोड़ता.
प्रश्न- मेरी मेरे माता-पिता से नहीं बनती. वे लोग चाहते हैं कि मैं आर्मी में जाने के रोज सुबह दौड़ने का अभ्यास करूं जबकि मैं संगीत सीखना चाहता हूं. मेरा गिटार भी उन लोगों ने तोड़ दिया है. मेरे पिताजी और चाचाजी वगैरह ऐसे लोग हैं जो हर समय पैसे, धंधे और नौकरी की बातें करते रहते हैं, मेरा यहां दम घुटता है. मैं क्या करूं ? -राज मल्होत्रा, मुंबई
उत्तर-माता-पिता को समझाना दुनिया का सबसे टेढ़ा काम है. उन्हें समझाने की कोशिश कीजिये कि न तो दौड़ने का अभ्यास करने से आजकल आर्मी में नौकरी मिलती है और न तैरने का अभ्यास करने से नेवी में. आप अपने मन का काम करना जारी रखिये. जाहिल लोगों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है चुपचाप अपना काम करना और उन्हें इग्नोर करना.
प्रश्न-मेरे पति अक्सर टूर पर बाहर रहते हैं. हमारी शादी को अभी सिर्फ दो साल हुये हैं और मुझे रात को उनकी बहुत कमी महसूस होती है. मेरा पड़ोसी कुंआरा है और हमेशा मेरी मदद को तैयार रहता है. मैं आजकल उसकी तरफ आकर्षित महसूस कर रही हूं. मैं खुद को बहकने से बचाना चाहती हूं, क्या करूं ? -क ख ग, दिल्ली
उत्तर-आप अपने पति को समझाइये कि वह अपने टूर की संख्या थोड़ी कम करें और आप अकेले में पूजा-पाठ और गायत्री मंत्र का जाप किया करें. अपने आप को संभालें वरना आपका सुखी परिवार देखते-देखते ही उजड़ जायेगा.
प्रश्न- मेरी उम्र 26 साल है और मेरे दो बच्चे हैं. मेरा मन अब सेक्स में नहीं लगता पर मेरे पति हर रात जिद करते हैं. मेरे स्तनों का आकार भी छोटा है जिसके कारण मेरे पति अक्सर मुझ पर झल्लाते रहते हैं. मैं क्या करूं ? -एक्सवाईजे़ड, अहमदाबाद
उत्तर-पति को प्यार से समझा कर कहिये कि शारीरिक कमी ईश्वर की देन है इसलिये उसके साथ सामंजस्य बनाएं. रात को बिस्तर पर पति को सहयोग करें, अगर सेक्स में मन नहीं लगता तो कुछ रोमांटिक फिल्में देखें और उपन्यास पढ़ें. इस उम्र में शारीरिक संबंधों से विरक्ति अच्छी नहीं.
प्रश्न.....प्रश्न....प्रश्न
उत्तर...उत्तर...उत्तर
चिंता की कोई बात नहीं. इन समस्याओं में से कितनी ठीक हुईं और कितनी नहीं, इसका मुझे कोई हिसाब नहीं रखना पड़ता. जी हां, मैं ही इन सवालों के जवाब देता हूं. मेरा नाम अनहदहै, मेरा कद पांच फीट चार इंच है और महिलाओं की इस घरेलू पत्रिका में यह मेरा दूसरा साल शुरू हो रहा है. मेरी शादी अभी नहीं हुई है और अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहेंगे तो आपको मेरे साथ सुबह पांच बजे उठ कर पानी भरना होगा और मेरे पिताजी का चिल्लाना सुनना होगा. ऐसा नहीं है कि वे सिर्फ मुझ पर चिल्लाते हैं. चिल्लाना दरअसल उनके लिये रोज़ की सैर की तरह है और वह इस मामले में मेरी मां और मेरे भाई में कोई फर्क नहीं करते. वह एक चीनी मिल में काम करते हैं, `हैं´ क्या थे लेकिन वे अपने लिये `थे´ शब्द का प्रयोग नहीं सुनना चाहते. उनका काम सुपरवाइज़र का है. मैं सुपरवाइज़र का मतलब नहीं जानता था तो यह सोचता था कि मिल पिताजी की है और हम बहुत अमीर हैं. वह बातें भी ऐसे करते थे कि आज उन्होंने दो मजदूरों की आधी तनख़्वाह काट ली है, आज उन्होंने एक कामचोर मजदूर को दो दिन के लिये काम से निकाल दिया या आज उनका मिल देर से जाने का मन है और वह देर से ही जाएंगे. जिस दिन वह देर से जाने के लिये कहते और देर से जागते तो मां कहती कि अंसारी खा जायेगा तुमको. वह मां को अपनी बांहों में खींच लेते थे और उनके गालों पर अपने गाल रगड़ने लगते थे. मां इस तरह शरमा कर उनकी बांहों से धीरे से छूटने की कोशिश करती कि वह कहीं सच में उन्हें छोड़ न दें. इस समय मां मेरा नाम लेकर पिताजी से धीरे से कुछ ऐसा कहतीं कि मुझे लगता कि मुझे वहां से चले जाना चाहिये. मैं वहां से निकलने लगता तो मुझे पिताजी की आवाज़ सुनायी देती, ``मैं राजा हूं वहां का, कोई अंसारी पंसारी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता.´´ मैं समझता कि मेरे पिताजी दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता. पिताजी वाकई किसी से नहीं डरते थे बस बाबा जब हमारे घर आते तभी मुझे पिताजी का सिर थोड़ा विनम्रता से झुका दिखायी देता. बाबा पिताजी के चाचाजी थे जो बकौल पिताजी पूरे खानदान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान थे. बाबा पिताजी से बहुत बड़े थे और दुनिया के हर सवाल का जवाब जानते थे. वे हमेशा कहते थे कि हमारा वक़्त आने वाला है और हम दोनों भाई इस बात का मतलब न समझते हुये भी खुश हो जाते थे.
बचपन सबसे तेज़ उड़ने वाली चिड़िया का नाम है
मैं या उदभ्रांत पिताजी को किसी दिन फैक्ट्री देर से जाने के लिये इसरार करते तो वह हमें गोद में उठाते, हमारे बालों को सहलाते और फिर नीचे उतार कर तेजी से अपनी सायकिल की ओर भागते. जिस दिन पिताजी फैक्ट्री नहीं जाते उस दिन मौसम बहुत अच्छा होता था और लगता था कि बारिश हो जायेगी लेकिन होती नहीं थी. हम चारों लोग कभी-कभी अगले मुहल्ले में पार्क में घूमने जाते और वहां बैठ कर पिताजी देर तक बताते रहते कि वह जल्दी ही शहर के बाहर आधा बिस्सा ज़मीन लेंगे और वहां हमारा घर बनेगा. फिर वह देर तक ज़मीन पर घर का नक्शा बनाते और मां से उसे पास कराने की कोशिश करते. मां कहती कि चार कमरे होंगे और पिताजी का कहना था कि कमरे तीन ही हों लेकिन बड़े होने चाहिए. वह तीन और चार कमरों वाले दो नक्शे बना देते और हमसे हमारी राय पूछते. हम दोनों भाई चार कमरे वाले नक्शे को पसंद करते क्योंकि उसमें हमारे लिये अलग-अलग एक-एक कमरा था. मां ख़ुश हो जाती और पिताजी हार मान कर हंसने लगते. पिताजी कहते कि वह हमें किसी दिन फिल्म दिखाने ले जाएंगे जब कोई फिल्म टैक्स फ्री हो जायेगी. मां बतातीं कि वह पिताजी के साथ एक बार फिल्म देखने गयी थी, उस फिल्म का नाम 'क्रांति'था और उसमें 'जिंदगी की ना टूटे लड़ी'गाना था. पिताजी यह सुनते ही मस्त हो जाते और 'आज से अपना वादा रहा हम मिलेंगे हर मोड़ पर...'गाना गाने लगते. उदभ्रांत मुझसे पूछता कि टैक्स फ्री फिल्म कौन सी होती है तो मैं अपने कॉलर पर हाथ रख कर बताता कि जिस फिल्म में बहुत बढ़िया गाने होते हैं उन्हें टैक्स फ्री कहते हैं. हम इंतज़ार करते कि कोई ऐसी फिल्म रिलीज हो जिसमें ख़ूब सारे अच्छे गाने हों.
पिताजी हमें हमेशा सपनों में ले जाते थे और हमें सपनों में इतना मज़ा आता कि हम वहां से बाहर ही नहीं निकल पाते. हम सपने में ही स्कूल चले जाते और हमारे दोस्त हमारी नयी कमीज़ें और मेरी नयी सायकिल को देखकर हैरान होते. मेरे दोस्त कहते कि मैं उन्हें अपनी सायकिल पर थोड़ी देर बैठने दूं लेकिन मैं सिर्फ नीलू को ही अपनी सायकिल पर बैठने देता. नीलू बहुत सुंदर थी. दुनिया की किसी भी भाषा में उसकी आंखों का रंग नहीं बताया जा सकता था और दुनिया का कोई भी कवि उसकी चाल पर कविता नहीं लिख सकता था. मैंने लिखने की कोशिश की थी और नाकाम रहा था. इस कोशिश में मैंने कुछ न कुछ लिखना सीख लिया था. इसी गलत आदत ने मुझे गलत दिशा दे दी और बीए करने के बाद मैंने पिताजी की सलाह मान कर बी'एड. नहीं किया और रात-दिन कागज़ काले करने लगा. लिखने का भूत मुझे पकड़ चुका था. नीलू मेरे देखते ही देखते दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो गयी थी, मेरा मुहल्ला दुनिया का सबसे खूबसूरत मुहल्ला और मैं दुनिया का सबसे डरपोक प्रेमी. मैंने उन रुमानी दिनों में हर तरह की कविताएं पढ़ी जिनमें एक तरफ तो शमशेर और पंत थे तो दूसरी तरफ मुक्तिबोध और धूमिल. हर तरह की कविता मुझे कुछ दे कर जाती थी और मैंने भी कविताई करते हुए ढेरों डायरियां भर डालीं.
मेरा लिखा कई जगह छप चुका था और मेरा भ्रम टूटने में थोड़ी ही देर बाकी थी कि मुझे लिखने की वजह से भी कोई नौकरी मिल सकती है. पत्रकारिता करने के लिये किसी पढ़ाई की ज़रूरत होने लगी थी. पत्रकारिता सिखाने के ढेर सारे संस्थान खुल चुके थे और जितने ज़्यादा ये संस्थान बढ़ते जा रहे थे पत्रकारिता ही हालत उतनी ही खराब होती जा रही थी. पता नहीं वहां क्या पढ़ाया जाता था और क्यों पढ़ाया जाता था. पिताजी की मिल (अब हमें उसे पिताजी की ही मिल कहने की आदत पड़ गयी है) के आस-पास की कई मिलें बंद हो चुकी थीं और इस मिल के भी बंद होने के आसार थे. कर्मचारियों को तनख़्वाहें कई महीनों से नहीं दी जा रही थीं और पिताजी ने मुझसे सिर्फ इतना कहा था कि मैं घर की सब्ज़ी और राशन का खर्चा संभाल लूं, वे उदभ्रांत की पढ़ाई के खर्चे का जुगाड़ कैसे भी करके कर लेंगे.
ये उन दिनों के कुछ आगे की बात है जब मैं और उदभ्रांत ज़मीन पर एक लकड़ी के टुकड़े से या पत्थर से एक घर का नक्शा बनाते जिसमें चार कमरे होते. बाबा ने उस मकान का नक्शा हमारे बहुत इसरार करने पर एक कागज़ पर बना कर हमें दे दिया था. हम ज़मीन पर बने नक्शे में अपने-अपने कमरों में जाकर खेलते. उदभ्रांत अक्सर अपने कमरे से मेहमानों वाले कमरे में चला जाता और मैं उसे पिताजी के कमरे में खोज रहा होता. एक बार तो ऐसा हुआ कि खेलते-खेलते मैं मेहमानों वाले कमरे में उदभ्रांत को पुकारता हुआ चला गया और वहां पिताजी अपने एक मित्र के साथ बातें कर रहे थे और उन्होंने मुझे उछल-कूद मचाने के लिये डांटा. उन्होंने मुझे डांटते हुये कहा कि घर में इतना बड़ा बरामदा है और तुम दोनों के अलग-अलग कमरे हैं, तुम दोनों को वहीं खेलना चाहिए, घर में आये मेहमानों को परेशान नहीं करना चाहिए. तभी बाबा ने आकर हमारे बड़े से नीले गेट का कुंडा खटकाया और मैंने उदभ्रांत ने कहा कि हमें पिताजी से कह कर अपने घर के गेट पर एक घंटी लगवानी चाहिए जिसका बटन दबाने पर अंदर `ओम जय जगदीश हरे´ की आवाज़ आये. बाबा अक्सर हमारे ही कमरे में बैठते थे और हमें दुनिया भर की बातें बताते थे. वे बाहर की दुनिया को देखने की हमारी आंख थे और हमें इस बात पर बहुत फख्र महसूस होता था कि हम दोनों भाइयों के नाम उनके कहने पर ही रखे गये थे वरना मैं `रामप्रवेश सरोज´ होता और मेरा छोटा भाई `रामआधार सरोज´. उनसे और लोग कम ही बात करते थे क्योंकि वे जिस तरह की बातें करते थे वे कोई समझ नहीं पाता. समझ तो हम भी नहीं पाते लेकिन हमें उनकी बातें अच्छी लगती थीं. हम जब छोटे थे तो हमारा काफ़ी वक़्त उनके साथ बीता था.
वह कहते थे कि जल्दी ही वो समय आयेगा जब हम सब गाड़ी में पीछे लटकने की बजाय ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे. हर जु़ल्म का हिसाब लिया जायेगा और हमारे हक हमें वापस मिलेंगे. हमें उनकी बातें सुन कर बहुत मज़ा आता. मुझे बाद में भी उतना समझ नहीं आता था लेकिन उदभ्रांत धीरे-धीरे बाबा के इतने करीब हो गया था कि उनसे कई बातों पर खूब बहस करता. पिछले चुनाव के बाद जब बाबा भंग की तरंग में नाचते-गाते पूरे मुहल्ले में मिठाई बांट रहे थे तो उदभ्रांत का उनसे इसी बात पर झगड़ा हो गया था कि उसने कह दिया था कि वह कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें पाल रहे हैं. बाबा ने बहस कर ली थी कि संविधान बनने के बरसों बाद हम गु़लामों को आज़ादी मिली है और उस पर नज़र नहीं लगानी चाहिये. बाबा जब बहस में उदभ्रांत से जीत नहीं पाते तो उसे थोड़ा इंतज़ार करने की नसीहत देते. ये बहसें अचानक नहीं थीं. जब वह छोटा था तो बाबा से हर मुद्दे पर इतने तर्कों के साथ बहस करता कि मैं उसे देख कर मुग्ध हो जाता. मैं उसकी बड़ी-बड़ी बातों वाली बहसों को देख कर सोचता कि ये ज़रूर अपनी पढ़ाई में नाम रोशन कर हमारे घर के दिन वापस लायेगा. मुझे पिताजी की बात याद आ जाती कि मुझे घर के कुछ खर्चे संभालने हैं ताकि उदभ्रांत अपनी पढ़ाई निर्विघ्न पूरी कर सके और हमारी उम्मीदों को पतंग बना सके.
तो घर के कुछ छोटे खर्चों को संभालने के लिये मैंने अपनी सारी ऊर्जा झोंक दी थी और कैसी भी एक नौकरी चाहता था.
नीला रंग भगवान का रंग होता है
ऐसे में `घर की रौनक´ नाम की उस पत्रिका में नौकरी लग जाना मेरे लिये मेरी ज़िंदगी में रौनक का लौट आना था. मैं शाम को मिठाई का डिब्बा लेकर नीलू के घर गया था तो वह देर तक हंसती रही थी. आंटी ने कह कि मैं छत पर जाकर नीलू को मिठाई दे आऊं. नीलू शाम को अक्सर छत पर डूबते सूरज को देखा करती थी. उसे आसमान बहुत पसंद था. उसे डूबते सूरज को देखना बहुत पसंद था. मेरे लिये यह बहुत अच्छी बात थी. मैं भी कभी उगा नहीं. मैं हमेशा से डूबता हुआ सूरज था.
``किस बात की मिठाई है साहब..?´´ वह पांचवीं क्लास से ही मुझे साहब कहती थी जब मैंने स्कूल के वार्षिकोत्सव में `साला मैं तो साहब बन गया´ गाने पर हाथ में पेप्सी की बोतल ले कर डांस किया था.
मैंने उसे सकुचाते हुए बताया कि मेरी नौकरी लग गयी है और यह नौकरी ऐसी ही है जैसे किसी नये शहर में पहुंचा कोई आदमी एक सस्ते होटल में कोई कमरा ले कर अपने मन लायक कमरा खोजता है. उसने पत्रिका का नाम पूछा. मैंने नाम छिपाते हुए कहा कि यह महिलाओं की पत्रिका है जिसमें स्वेटर वगैरह के डिजाइनों के साथ अच्छी कहानियां और लेख भी छपते हैं. उसके बार-बार पूछने पर मुझे बताना ही पड़ा. उसकी हंसी शुरू हुई तो लगा कि आसमान छत के करीब आ गया. मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी नौकरी देश की किसी अच्छी और बड़ी पत्रिका में नहीं लगी. मुझे नौकरी से ज़्यादा उसकी हंसी की ज़रूरत थी. नौकरी की भी मुझे बहुत ज़रूरत थी. नौकरी देने वाले ये नहीं जानते थे कि नौकरी की मुझे हवा से भी ज़्यादा ज़रूरत थी और नीलू इस बात से अंजान थी कि उसकी हंसी की मुझे नौकरी से भी ज़्यादा ज़रूरत थी.
प्रश्न- मैं अपने पड़ोस में रहने वाली लड़की से बचपन से प्यार करता हूं. हम दोनों दोस्त हैं लेकिन उसे नहीं पता कि मैं उसे प्यार करता हूं. वह दुनिया की सबसे खूबसूरत हंसी हंसती है. उसकी हंसी सुनने के लिये मैं अक्सर जोकरों जैसी हरकतें करता रहता हूं और उसकी हंसी को पीता रहता हूं. मैं चाहता हूं कि मैं ज़िंदगी भर उसके लिये जोकरों जैसी हरकतें करता रहूं और वह हंसती रहे. लेकिन मैं उससे अपने प्यार का इज़हार करने में डरता हूं, कहीं ऐसा न हो कि मैं उसकी दोस्ती भी खो दूं और ज़िंदगी उसकी हंसी सुने बिना बितानी पड़े. मैं क्या करूं ?
मैं अक्सर कई सवालों के जवाब नहीं दे पाता. पत्रिका में छापने लायक जवाब तो कतई नहीं. मैं ऐसे पाठकों को व्यक्तिगत रूप से उत्तर देता हूं और उनसे सुहानुभूति जताता हूं कि मेरे पास हर प्रश्न का कोई न कोई उत्तर ज़रूर है और मैं उनके लिये दुआ करुंगा. मैं यह भी सोचता हूं कि जिन सवालों के जवाब मुझे न समझ में आयें उन्हें लोगों के बीच रख दूं और कोई ऐसा विकल्प सोचूं कि अनुत्तरित सवालों को समाज के सामने उत्तर के लिये रखा जा सके. लेकिन मेरी पत्रिका में ऐसी कोई व्यवस्था सोचनी भी मुश्किल है, मैं जब अपनी पत्रिका निकालूंगा तो ज़रूर एक ऐसा कॉलम शुरू करुंगा.
ऑफिस में मुझे उप-सम्पादक की कुर्सी पर बिठाया गया था और मैं वहां सबसे कम उम्र का कर्मचारी था. पत्रिका के ऑफिस जा कर मुझे पता चला कि जिन लोगों के बाल सफ़ेद होते हैं उनकी हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिये क्योंकि वे कभी गलत नहीं होते. कि सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला आदमी सबसे बुद्धिमान होता है और उससे कभी बहस नहीं की जानी चाहिये. कि नौकरी चाहे किसी पत्रिका में की जाये या किसी किराने की दुकान में, अंतत: दोनों को करने के लिये नौकर ही होना पड़ता है. पत्रिका में लगभग सारे लोग पुराने थे जिनमें संपादकीय विभाग में काम करने वाले लोगों यानि दीन जी, दादा, गोपीचंद जी, मिस सरीन आदि को मुख्य माना जाता था. मुख्य संपादक कहा जाने वाला आदमी वैसे तो दीन और दादा से कम उम्र का था लेकिन इन दोनों की चमचागिरी उसे बहुत भाती थी और दो लगभग बुज़ुर्गों से मक्खनबाज़ी करवाने में उसे खुद में बड़ा-बड़ा सा महसूस होता था.
कुछ ही समय में मैं इस नौकरी से बहुत तंग आ गया. घर के राशन और सब्ज़ी के ख़र्च वाली बात पिताजी ने मुझसे तब कही थी जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था और मेरे लिये नौकरी बहुत दूर की बात थी. इस बात को सात साल हो चुके हैं और अब जा कर पिछले कुछ समय से ही मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर पा रहा हूं और इस बात को लेकर मैं इतना शर्मिंदा हूं कि इस नौकरी को छोड़ कर दूसरी नौकरी खोजने का खतरा नहीं उठा सकता, और ये नौकरी इतना समय कभी नहीं देती कि मैं दूसरी जगह इंटरव्यू देने की सोच भी सकूं.
पत्रिका ने मुझे वैसे तो सब-एडिटर का ओहदा दिया था लेकिन करना मुझे बहुत कुछ पड़ता था. सबसे बुरा और उबाऊ काम था कवि दीनदयाल तिवारी `दीन´ के लिखे लेखों की प्रूफ रीडिंग करना. तिवारी जी ऑफिस में सबसे सीनियर थे और हमेशा 'आशीर्वाद'को 'आर्शीवाद'और 'परिस्थिति'को 'परिस्थिती'लिखते थे. 'दीन'उनका उपनाम था जिससे वह कविता लिखकर उसे सुनाने की रणनीतियां बनाया करते थे. गो वह मुझसे अपने लेखों की चेकिंग करवाते समय यह कहते थे कि इससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा और जो एकाध मिस्प्रिन्तिंग हो गयी है वह ठीक हो जायेगी. जब मैं उनके लेखों को चेक करता रहता तो वह अपनी बेटी के मेधावीपने और उसके पढ़ाई में पाये पुरस्कारों के बखान करते रहते. बातों-बातों में वह मुझसे मेरी शादी के बारे में पूछने लग जाते और मैं अक्सर ऑफिस के बाहर की दीवारों को घूरने लगता. दीवारें नीली थीं. नीलू अक्सर नीले रंग के कपड़े पहनती थी. नीला मेरा पसंदीदा रंग था.
``नीला रंग भगवान का रंग होता है.´´ वह छोटी थी तो अक्सर कहती. उस समय वह नीली फ्रॉक पहने होती थी. मैं उससे पूछता कि उसे यह कैसे पता तो वह अपनी उंगली ऊपर उठा कर आसमान की ओर दिखाती थी.
`´आसमान नीला होता है और समन्दर भी. जो अनंत और सबसे ताक़तवर चीज़ें हैं वह नीली ही हो सकती हैं.´´ मैं उस समय भी उसकी फ्रॉक को देखता रहता था. वह बोलती थी तो उसकी आंखें खूब झपका करती थीं और इसके लिये उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती थीं. उनका कहना था कि यह बहुत गंदी आदत है और उसे तुरंत इस आदत को बदल लेना चाहिये.
शुक्र है उसकी यह आदत अब भी थोड़ी बहुत बरक़रार है. और मुझसे बात करते हुये उसकी आंखें आज भी उसी तरह मटकती और झपकती हैं. मैं अक्सर उसकी ओर देखता रहता हूं और उसकी बातें कई बार नहीं सुन पाता. जब वह टोकती है और मैं जैसे नींद से जागता हूं तो वह कहती है, ``अच्छा तो साहब का टॉवर चला गया था ?´´ मैं झेंप जाता हूं. वह खिलखिलाती हुई पूछती है, ``अब नेटवर्क में हो? अब पूरी करूं अपनी बात?´´ मैं थोड़ा शरमा कर थोड़ा मुस्करा कर फिर से उसकी बात सुनने लगता हूं लेकिन दुबारा उसकी आवाज़ और आंखों में खोने में मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं लगता. उसका कहना है कि मैं ऐसे रहता हूं कि मेरा कुछ बहुत क़ीमती खो गया है और किसी भी वक़्त मेरा टॉवर जा सकता है. एक बार जब वह पांचवी क्लास में थी, वह अपनी टीचर के घर से एक खरगोश का बच्चा लायी थी जो पूरी देखभाल के बावजूद सिर्फ चार दिनों में मर गया. नीलू की आंखें रो कर भारी हो गयी थीं. उसके बाद उसके बहुत रोने पर भी उसकी मां ने दुबारा कोई जानवर नहीं पाला, खरगोश के बारे में तो बात भी करना उसके लिये मना हो गया. खरगोश सफ़ेद था और उस दिन नीले आसमान का एक छोटा सा हिस्सा सफ़ेद हो गया था. नीलू उसे ही देर तक देखती रही थी. नीले रंग का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व था. मेरी और नीलू की पहली मुलाक़ात मुझे आज भी वैसी की वैसी याद है. मैं तीसरी क्लास में था और नीलू का एडमिशन इसी स्कूल में तीसरी क्लास में हुआ. उसके पिताजी का ट्रांसफर इस शहर में होने के कारण यह परिवार इस शहर में एक किराये के कमरे में आया था जिसे छोड़ कर बाद में वो लोग अपने नये खरीदे मकान में कुछ सालों बाद शिफ्ट हुए.
तो नीलू ने स्कूल ड्रेस की नीली फ्रॉक पहनी थी और अपनी मम्मी की उंगली पकड़े स्कूल की तरफ आ रही थी. स्कूल में प्रार्थना शुरू हो चुकी थी. मैं अकेला स्कूल जाता था क्योंकि पिताजी सुबह-सुबह फैक्ट्री चले जाते थे. मुझे उस दिन स्कूल को देर हो गयी थी और मैं तेज़ कदमों से जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुंचा था मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी. पीछे पलट कर देखा तो नीलू बार्बी डॉल जैसी नीले ड्रेस में रोती हुयी स्कूल की तरफ आ रही थी. उसकी मम्मी उसे कई बातें कह कर बहला रही थीं जैसे वह उसके साथ अपना भी नाम तीसरी क्लास में लिखा लेंगी और रोने का गंदा काम के.जी. के बच्चे करते हैं और तीसरी क्लास के बच्चों को समझदार होना चाहिये. मैं भूल गया कि मुझे देर हो रही है और मेरे कदम गेट पर ही रुक गये. जब नीलू मम्मी का हाथ पकड़े गेट पर पहुंची तो गेट में घुसने से पहले उसकी नज़र मुझ पर पड़ी जो उसे एकटक देखे जा रहा था. वह अचानक रुक गयी और उसने आगे बढ़ी जा रही अपनी मम्मी को हाथ खींच कर रोका.
``क्या है नीलू ?´´ आंटी ने झल्लाहट भरी आवाज़ में पूछा था.
``उसका ब्लू देखो, मुझे वैसा ब्लू चाहिये. मैं ये वाली फ्रॉक कल से नहीं पहनूंगी.´´ उसने मेरी पैण्ट की और इशारा कर कहा था और फिर से सुबकने लगी थी. उसकी मम्मी ने उससे वादा किया कि वह उसे मेरे वाले नीले रंग की फ्रॉक कल ही बनवा देंगी.
घर आ कर मैंने पहली बार अपनी पैण्ट को इतने ध्यान से देखा और मुझे उस पर बहुत प्यार आया. मैंने उस दिन मम्मी को अपनी पैण्ट नहीं धोने दी और पहली बार अपनी कपड़े ख़ुद धोये. बाद में पता चला कि जब वह छोटी थी और बोलना भी नहीं सीखा था तब से उसे सिर्फ़ नीले रंग से ही फुसलाया जा सकता था. उसे गोद में ले कर बाहर घुमाने जाने वाले को नीली कमीज पहननी पड़ती थी और उसके इस स्वभाव के कारण उसका नाम नीलू रखा गया. बाद में घर वालों ने स्कूल में उसका नाम अर्पिता रखा था लेकिन उसने बिना घर वालों को बताये हाईस्कूल के फॉर्म में नीलू भर दिया था. वो कमाल थी.
दीन जी के हिस्से का काम भी मुझे सिर्फ़ इसलिये करना पड़ता है कि मेरी उम्र सबसे कम है. उनका काम करने के एवज़ में वह मुझ पर दोहरा अत्याचार करते हुये मुझे अपनी ताज़ा बनायी हुई कुछ कविताएं भी सुना डालते हैं. उनकी कविताओं में भूख, भूमंडलीकरण, बाज़ार और किसान शब्द बार-बार आते हैं और इस बिनाह पर वह मुझसे उम्मीद रखते हैं कि मैं उनकी कविताओं को सरोकार वाली कविताएं कहूं. उनकी कविताएं हमारी ही पत्रिका में छपती हैं जिसके बारे में उनका कहना है कि अगर अपने पास पत्रिका है तो फिर दूसरों को क्यों ओब्लाइज किया जाये. उनके पास अपनी कविताओं पर मिले कुछ प्रशंसा पत्र भी हैं जिनकी प्रतिक्रियास्वरूप अब वह एक कहानी लिखने का मन बना रहे हैं जिसका नाम वह ज़रूर `भूखे किसान´ या `भूखा बाज़ार´ रखेंगे.
मुझसे पहले प्रश्न उत्तर वाला कॉलम सम्पादक दिनेश क्रांतिकारी खुद देखता था और उत्तरों को बहुत चलताऊ ढंग से निपटाया जाता था. जब उसने मुझे यह ज़िम्मेदारी दी तो ऑफिस में सब पता नहीं क्यों मंद-मंद मुस्करा रहे थे. मैंने इसे एक बड़ी ज़िम्मेदारी समझ कर लिया था और लोगों की समस्याएं पढ़ते हुये मुझे वाकई उनसे सुहानुभूति होती थी. जल्दी ही मुझे लगने लगा कि मेरा यह मानसिक उलझनें सुलझाने वाला `मैं क्या करूं´ नाम का कॉलम और लोगों के लिये मज़ाक का सबब है. मैंने हर प्रश्न का उत्तर देने में अपनी पूरी ईमानदारी बरती है और कई बार ऐसा हुआ है कि प्रश्न का उत्तर न समझ में आने पर मैंने अपने फोन से किसी सेक्सोलॉजिस्ट या किसी मनोवैज्ञानिक से बात की है और उनके मार्गदर्शन से पाठक की समस्या का समाधान करने की कोशिश की है.
लेकिन अब चीज़ें बहुत हल्की हो गयी हैं. दीन जी के साथ चौहान साहब और दासगुप्ता जी यानि डिजाईनर दादा भी मुझसे मज़े लेने की फि़राक में रहते हैं. अभी कल ही मैं ऑफिस से निकल रहा था कि दादा ने मुझे अपने पास बुला लिया और बोले, ``मेरी पत्नी जब भी मायके जाती है, मेरा मन सामने वाली अंजुला बनर्जी की तरफ़ भागता है. दिन तो कट जाता है मगर रात नहीं कटती. मुझे लगता है वो भी मुझे पसंद करती है. मैं क्या करूं ?´´
मुझे झल्लाहट तो बहुत हुई और मन आया कि कह दूं कि बुड्ढे अपनी उमर देख लेकिन वह बॉस के सबसे करीबी लोगों में माने जाते हैं इसलिये मैंने मन मार कर कहा कि दादा आप भाभीजी को मायके मत जाने दिया करें. मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग अपने घरों में अपने बच्चों के सामने कैसे सहज रहते होंगे. दादा के साथ दीन जी भी हंसने लगे और अपनी नयी कविता के लिये एकदम उपयुक्त माहौल देख कर दे मारी.
उनके बिना रात काटना वैसा ही है
जैसे रोटी के बिना पेट भरने की कल्पना
जैसे चांद के बिना रात और जैसे सचिन के बिना क्रिकेट
वह आयें तो बहार आये और वह जायें तो बहार चली जाये
मगर हम हार नहीं मानेंगे
कहीं और बहार को खोजेंगे
गर उनके आने में देर हुयी
तो बाहर किसी और को .......
बाद के शब्द और लाइनें सुनाने लायक नहीं थीं. दादा ने कहा कि कुछ शब्द अश्लील हैं तो उनका कहना था कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अश्लील है और अगर हम जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में कविता न लिखें तो वह कविता झूठी है. कविता को नयी और विद्रोही भाषा की ज़रूरत है. मैंने यह कहने की सोची की इस भाषा में सिर्फ़ आप ही बात करते हैं लेकिन कह नहीं पाया. उनके बाल सफे़द थे और उनका अनुभव मुझसे ज़्यादा था जिससे दुनिया में यह मानने का प्रचलन था कि उनमें और मुझमें कोई तुलना होगी तो मैं ही हमेशा गलत होउंगा. सफेद बालों वाले लोग किसी भी बहस में हारने पर अपने सफेद बालों का वास्ता दिया करते थे और यह उम्मीद करते थे कि अब इस अकाट्य तर्क के बाद बहस उनके पक्ष में मुड़कर ख़त्म हो जानी चाहिए.
मैं जब नीलू के घर पहुंचा तो वहां काफ़ी चहल-पहल थी. मुझे देखते ही आंटी ने मुझसे दौड़ कर थोड़ी और मिठाई लेकर आने को कहा. उन्होंने कहा कि एक ही तरह की मिठाई आई है और उन्हें काजू वाली बर्फी चाहिये. मैं बर्फी लेकर पहुंचा तो पता चला कुछ मेहमान आये थे और सब उनकी खातिरदारी में लगे थे. मैं मिठाई देकर थोड़ी देर खड़ा रहा कि कोई अपने आप मुझे नीलू का पता बता दे. हॉल में टीवी चालू था और उसे कोई नहीं देख रहा था. उस पर एक विज्ञापन आ रहा था जिसे देख कर मेरे होंठों पर मुस्कराहट आ गयी. `जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों का जब सजाना हो, नेरोलक नेरोलक....´. मुझे यह भी याद आया कि हमारे घर में चूना होने का काम पिछले तीन दीवालियों से टलता आ रहा है. शायद अगली दीवाली में मैं और उद्भ्रांत अपने हाथ में कमान लेकर चूना पोतने का काम करें और अपने छोटे से कमरे को सफ़ेद रंग में नील डालकर रंग डालें.
आंटी मेरे पास आकर खड़ी हुईं और इस नज़र से देखा जैसे मिठाई देकर वापस चले जाना ही मेरा फ़र्ज़ था. मैंने नीलू के बारे में पूछा तो उन्होंने छत की ओर इशारा किया और मुझे हिदायत दी कि मैं जल्दी उसे लेकर नीचे आ जाऊं. मैं छत पर पहुंचा तो नीलू अपना पसंदीदा काम कर रही थी. उसका आसमान देखना ऐसा था कि वह किसी से बात कर रही थी.
``आओ साहब. कैसे हो ?´´ उसने सूनी आंखों से पूछा.
``नीचे भीड़ कैसी है ?´´ मैंने उसके बराबर बैठते हुये पूछा.
``कुछ नहीं, मां के मायके से कुछ लोग आये हैं मुझे देखने......´´ मेरा दिल धक से बैठ गया. मेरे मन में एक पाठक का सवाल कौंध गया, ``मैं जिस लड़की से प्यार करता हूं वह मुझे बचपन से जानती है. मुझे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त कहती है लेकिन मैं उसे बचपन से चाहता हूं. मैं उसे इस डर से प्रपोज नहीं करता कि कहीं मैं उसकी दोस्ती खो न दूं. मैं क्या करूं ?´´ मैंने ऐसे कई जवाबों के व्यक्तिगत रूप से देने के बाद कल ही पत्रिका में एक जवाब दिया था. मैंने उसके जवाब में लिखा था कि उसे इतना रिस्क तो लेना ही पडे़गा. लेकिन मैं जानता हूं किसी को कुछ करने के लिये कह देना और खुद उस पर अमल करना दो अलग-अलग बातें हैं. हम दोनों एक दूसरे के हमेशा से सबसे क़रीब रहे हैं और अपन सारी बातें एक दूसरे से बांटते रहे हैं. लेकिन कभी शादी और एक दूसरे के प्रति चाहत का इज़हार...कम से कम मेरे हिम्मत से बाहर की चीज़ है.
``कौन है लड़का..?´´ मेरे गले से मरी सी आवाज़ निकली. उसने बताया कि उसकी मम्मी की बहन की ननद का लड़का है और इंजीनियर है. मुझे अपने उन सभी पाठकों के पत्र याद आ गये जिनकी प्रेम कहानियों के खलनायक इंजीनियर हैं. कितने इंजीनियर होने लगे हैं आजकल ? सब लोग आ गये हैं और वह कल आयेगा.
``मीनू बता रही थी बहुत लम्बा है लड़का.´´ उसने मेरी ओर देखते हुये कहा. उसकी आंखें बराबर मटक रही थीं और पलकें खूब झपक रही थीं.
``लम्बे लड़कों में ऐसी क्या ख़ास बात होती है ?`` मैंने अपने सवाल की बेवकूफ़ी को काफ़ी नज़दीक से महसूस किया.
``होती है ना, वे जब चाहें हाथ बढ़ा कर आसमान से तारे तोड़ सकते हैं.´´ उसने फिर से नज़रें आसमान की ओर उठा दीं.
``तारे तोड़ने के लिये तो मैं तुम्हें गोद में उठा लूं तो भी तोड़े ही जा सकते हैं. आखिर कितनी हाइट चाहिये इसके लिये....´´ मैंने कुछ पल थम कर धीरे से कहा. यह वाक्य मेरे आत्मविश्वास को अधिकतम पर ला कर खींचने का नतीजा था.
``तो कब उठाओगे साहब जब आसमान के सारे तारे टूट जायेंगे तब...?´´ उसने पलकें मटकायीं. मुझे न तो अपने कहे पर विश्वास हुआ था और न उसकी बात पर जो मेरे कानों तक ऐसे पहुंची थी मानों मैं किसी सपने में हूं और बहुत दूर निकल चुका हूं. उसकी आवाज़ रेशम सी हो गयी थी और आसमान का रंग काले से नीला हो गया था. मैंने हिम्मत करके उसकी हथेली पर अपनी हथेली रख दी.
``आसमान का रंग बदल रहा है न ?´´ मैंने उससे पूछा.
``हां साहब, आसमान का रंग फिर से नीला हो रहा है. पता है नीले रंग की चीज़ें जीवन देती हैं.´´ उसने मेरी हथेली पर अपनी दूसरी हथेली रखते हुये कहा. मेरे सामने बहुत सारे दृश्य चल रहे थे. मेरी नयी सायकिल जो कभी खरीदी नहीं गयी और उस पर बैठी हुयी नीलू. नीलू के फ्रॉक में जड़े ढेर सारे सितारे जो धीरे-धीरे बिखर कर आसमान में उड़ रहे हैं. मैं उन्हें फिर से पकड़ कर नीलू की फ्रॉक में टांक देना चाहता हूं. मैं जैसे एक सपने में दूसरा सपना देखने लगा हूं.
``तुम्हारे पास नीली साड़ी है ?´´ मैंने अपनी आवाज़ इतने प्यार से उसे दी कि कहीं टूट न जाये. उसकी आवाज़ भी शीशे जैसी थी जिस पर `हैंडल विद केयर´ लिखा था.
``बी. एड. वाली है न....लेकिन वह बहुत भारी है साहब. तुम मेरे लिये एक सपनों से भी हल्की साड़ी ले आना.´´
``तुम सिर्फ़ नीला रंग पहना करो नीलू.´´
``मैं सिर्फ़ शाम को नीले रंग पहनना चाहती हूं साहब क्योंकि दिन में तुम आते ही नहीं.´´
``मैं कहीं जाउंगा ही नहीं कि मुझे वापस आना पड़े. मुझे कहीं जाने में डर लगता है क्योंकि मुझे लौट कर तुम्हारे पास आना होता है.`` मैंनें उसकी हथेलियां महसूस कीं. मुझे डर लगा कि उसके घर का कोई छत पर आ न जाय.
``मुझे कुछ कहना है तुमसे साहब.`` उसने रेशम सी धीमी आवाज़ में कहा
``क्या...?´´
``उसके लिये मुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी. मैं आंखें बंद करती हूं, तुम मेरी ओर देखते रहना. मेरी आंखों में देखोगे तो तुम्हारा टॉवर चला न जाये इसलिये....´´ उसने मुस्करा कर अपनी आंखें बंद कीं और मैंने उसकी हथेलियां थाम लीं. उसका नर्म हाथ थामते हुये मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी को उसकी हाथ की तरह की कोमल और नर्म होना चाहिये. मैं उसकी हथेलियां थामे बैठा रहा और वह कहती रही. नया साल मेरे लिये दुनिया की सबसे बड़ी ख़ुशी लेकर आया था. मैंने मन में सेाचा कि कल ही वह प्यारा सा कार्ड इसे दे दूंगा जो मैं इस साल उसे देने और अपने दिल की बात कहने के लिये लाया था...साथ ही पिछले सालों के भी अनगिनत कार्ड.
``तुम अगर कभी कोई सायकिल खरीदना तो मुझे उस पर बिठाना और हम दोनों जंगल में खरगोश देखने चलेंगे. जब तुम्हें कुछ लिखने का मन करेगा तो मैं तुम्हारे सामने बैठ जाउंगी और अपनी आंखें बंद कर लूंगी ताकि तुम मुझे देखते हुये टॉवर में रहकर कुछ ऐसा लिखो कि उसके बाद जीने की कमी भी पड़ जाये तो कोई ग़म न हो. तुम जब कोई कविता लिखना तो ऐसा लिखना कि उसे छुआ जा सके और उसे छूने पर या तो बहुत जीने का मन करे या फिर दुनिया को छोड़ देने का....तुम हमेशा नीले रंग में लिखना.....´´
वह बोलती जा रही थी और मुझे पहली बार पता चला कि मैं उसकी आंखों में ही नहीं खोता था. उसके चेहरे से जो नीली मुकद्दस रोशनी मेरी हथेलियों पर गिर रही थी मैं उसमें भी ऐसा खो गया था कि मुझे उसकी आवाज़ किसी सपने से आती लग रही थी. अब मुझे कोई डर नहीं था कि उसके घर से कोई छत पर आ जायेगा. उसके घर में कोई नहीं था. मुहल्ले में कोई नहीं था. पूरी दुनिया में कोई नहीं था.
हम एक नीले सपने में थे और आसमान का रंग रात में भी नीला था.
मुझे बैठने के लिये एक क्यूबिकल जैसा कुछ मिला था जिसे तीन बाई तीन का कमरा भी कहा जा सकता था क्योंकि उसकी बाक़ायदा एक छत थी और एक बड़ी सी खिड़की भी. उसे देख कर लगता था कि इसे बाथरुम बनवाने के लिये बनाया गया होगा और बाद में किसी वास्तुशास्त्री के कहने पर स्टोर रूम में रूप में डेवलप कर दिया गया होगा. कमाल यह था कि बाहर से देखने पर यह सिर्फ़ एक खिड़की दिखायी देती थी और अंदाज़ा भी नहीं हो पाता था कि इस खिड़की के पीछे एक कमरे जैसी भी चीज़ है. इसका दरवा़जा पिछली गली में खुलता था और हमेशा बंद रहता था. ऑफि़स में घुसने के बाद खिड़की ही इसमें घुसने का एक ज़रिया थी और जब मैं उछल कर खिड़की के रास्ते अपने केबिन में दाखिल होता था तो चोर जैसा दिखायी देता था. जब सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो गेट पर ही दीन जी मिले और सिगरेट का धुंआ छोड़ते हुये उन्होंने मेरी चुटकी ली.
``सर, मेरी उम 56 साल है. मुझे अपने ऑफिस की एक लड़की से इश्क हो गया है जो सिर्फ़ 22-23 साल की है. मैं उसका दीवाना हो रहा हूं और उससे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं लेकिन वह मुझे अंकल कहती है. मैं उसे कैसे अपना बनाऊं ?´´ मैंने देखा दीन के चेहरे पर शर्म संकोच के कहीं नामोनिशान तक नहीं थे. क्या इस उम्र के सारे बुड्ढे ऐसे ही होते हैं ? क्या घर पर ये अपनी बेटी को भी इसी नज़र से देखता होगा ? आखिरकार इसने पूरी उम्र किया क्या है जो इसकी उम्र इतनी तेज़ी से निकल गयी है कि इसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ. इसी समय इत्तेफ़ाक हुआ कि मिस सरिता सरीन ऑफिस में दाखिल हुईं और दरवाज़े पर हमारा अभिनंदन करके अंदर चली गयीं.
``हैलो अनहद, हैलो अंकल.´´
दीन जी का मेरा मज़ाक उड़ाने का पूरा बना-बनाया मूड चौपट हो गया और वह दूसरी ओर देख कर दूसरी सिगरेट जलाने लगे.
मैं अंदर पहुंचा तो एक और आश्चर्य मेरे इंतज़ार में था. मेरे केबिन कम दड़बे की खिड़की पर पता नहीं कोयले से या किसी मार्कर से मोटे-मोटे हर्फों में लिखा था ``उत्तर प्रदेश´´. मैंने उसे मिटाने का कोई उपक्रम नहीं किया और कूद कर अंदर चला गया. मेरी मेज़ पर ढेर सारे प्रश्न पडे़ थे जिनके उत्तर मुझे देने थे. उस दिन के बाद से मेरे केबिन को `उत्तर प्रदेश´ के नाम से जाना जाने लगा बल्कि कहा जाये तो उस खिड़की का नाम `उत्तर प्रदेश´ रख दिया गया था. मुझे सर्कुलेशन और सबक्रिप्शन विभाग से पता चला कि मेरे कॉलम की खूब तारीफ़ें हो रही हैं और इसकी वजह से पत्रिका की बिक्री भी बढ़ रही है लेकिन इस खबर का अपने हक में कैसे उपयोग करना है, मुझे समझ में नहीं आया. हां, यह ज़रूर हुआ कि दीन जी और दादा के अलावा मिस सरीन, गोपीचंद, और एकाध बार तो मेरे संपादक भी (पीने के बाद जोश में आ कर) एकाधिक बार मेरे केबिन में आये और अपने-अपने प्रश्नों के उत्तर जानने चाहे. मिस सरीन ने एक बार पूछा- ``सर मेरी समस्या यह है कि मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं और मैं अभी शादी नहीं करना चाहती. मुझे अपना कैरियर बनाना है और जीवन में बहुत आगे जाना है. मैं शादी जैसी चीज़ में विश्वास नहीं करती. मैं क्या करूं ?´´ मैं थोड़ी देर तक उनकी मुस्कराहट को पढ़ने की कोशिश करता रहा और जब मुझे लगा कि मज़ाक में ही सही, वह इस प्रश्न का उत्तर चाहती हैं तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शादी कोई रुकावट नहीं होती, सारी रुकावटें दिमाग में होती हैं और इन्हें अगर जीत लिया जाये...... मेरी बात खत्म होने से पहले ही दीन जी और दादा दरवाज़े पर आकर खड़े हो गये और चिल्ला-चिल्ला कर हंसने लगे. मैं झेंप गया और सरीन अपनी कुर्सी पर चली गयीं.
एक रात जब मुझे निकलने में थोड़ी देर हो गयी थी और सम्पादक महोदय के केबिन में तरल-गरल का दौर शुरू हो चुका था कि मेरी खिड़की पर खटखट हुयी. मैंने देखा तो मेरे सम्पादक लड़खड़ाते हुये मेरी खिड़की पर खड़े थे. मैं तुरंत एक फौजी की तरह उठा और मैंने सैल्यूट भर नहीं मारा.
``यार अनहद, मेरी बीवी अक्सर मुझे बिस्तर पर नाकाम होने के लिये ताने मारती है यार. मैंने कई दवाइयां करके देख लीं, मुझे लगता है इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण है, तुम कुछ बता सकते हो ?´´ मैं अभी कुछ सोच ही रहा था कि मेरे आदरणीय सम्पादक महोदय ने अपनी पैण्ट की जिप खोल ली और एक घिनौनी हरकते करते हुये बोले, ``देखो तो कोई कमी तो नहीं दिख रही ना, शायद कोई मनोवैज्ञानिक कारण होगा.....´´ मैंने नज़रें चुराते हुये कहा, ``हो सकता है सर.´´ वे पूरी रौ में थे, ``यार इसको टेस्ट कर लेते हैं, ज़रा कूद के बाहर आओ और मिस सरीन को फोन करके कहो न कि सर ने बुलाया है ज़रूरी काम है....आज इसकी टेस्टिंग उस पर ही कर लेते हैं. साला मेरी बूढ़ी बीवी से सामने सर ही नहीं उठाता और सरीन का नाम लेते ही देखो फन उठाये खड़ा है.´´ अपनी कही गयी इस मनमोहक बात पर उन्हें खुद इतना मज़ा आया कि वह हंसते-हंसते ज़मीन पर ही बैठ गये. उस समय दीन जी मेरे लिये तारणहार बन कर आये और दादा के साथ आ कर उनको उठाया और सीट पर बिठाया. मैं अगले पांच मिनटों में अपना काम समेट कर वहां से निकल गया.
पिताजी का रूटीन हो गया था कि सुबह नहा-धो कर खा-पी कर बंद फैक्ट्री के लिये ऐसे निकलते थे जैसे काम पर ही जा रहे हों. भले ही जा कर फैक्ट्री के बंद फाटक पर धरना ही देना हो, उन्हें देर कतई मंजूर नहीं थी. फैक्ट्री के सभी मज़दूर फाटकों पर धरने पर बैठते और शाम तक किसी चमत्कार का इंतज़ार करते. यह चीनी मिल 90 साल पुरानी थी जिसे नूरी मियां की मिल कहा जाता था. मिल के शुरू होने के कुछ दिन बाद नूरी मियां का इंतकाल हो गया और इसे कुछ दशकों बाद तत्कालीन सरकार ने नूरी मियां के परिवार की रज़ामंदी से अधिगृहित कर लिया था. अच्छी-खासी चलती मिल को पिछली प्रदेश सरकार ने बीमार मिल बता कर इस पर ताला डाल दिया था. सरकारें हर जगह ताला डाल रही थीं और पता नहीं इतने ताले कहां से लाये जाते थे क्योंकि अलीगढ़ में तो तालों का कारोबार कम होता जा रहा था, वहां और कारोबार बढ़ने लगे थे. पिताजी और सभी मज़दूर पिछले सात साल से इस उम्मीद में धरने पर बैठे थे कि कभी तो मिल चालू होगी और कभी तो वे फिर से अपने पुराने दिनों की झलक पा सकेंगे. लेकिन इस सरकार के फरमान से उनकी रही-सही हिम्मत डोलने लगी थी.
एक दिन धरने वाली जगह पर अंसारी पहुंच गया और सभी मज़दूरों ने उसे घेर लिया. सबने उससे अपने दुखड़े रोने शुरू किये तो वह खुद वहीं धम से बैठ गया और रोने लगा. उसने पिताजी के कंधे पर हाथ रखा और सुबकने लगा. पिताजी सहित सभी मज़दूरों ने अपने मालिक का यह रूप पहली बार देखा था. उन्हें नया-नया लगा और वे और क़रीब खिसक आये. अंसारी ने रोते-रोते टूटे-फूटे शब्दों में जो कुछ बताया वह मज़दूरों की समझ में पूरी तरह से नहीं आ सकता था लेकिन पिताजी सुपरवाइज़र थे और उन्हें लगता था कि सुपरवाइज़र होना दुनिया का सबसे बड़ा ज़िम्मेदारी का काम है. उनका मानना था कि सुपरवाइज़र को सब कुछ पता होना चाहिये. पता नहीं वह अंसारी की बातों के कितने टुकड़े समेट पाये थे और हम तक जो टुकड़े उन्होंने पहुंचाये उनमें कितनी सच्चाई थी और कितना उनका अंदाज़ा. मैं उनकी किसी भी बात की सत्यता का दावा नहीं पेश कर रहा लेकिन उनकी बातें बताना इसलिये ज़रूरी है कि उस दिन पिता को पहली बार इतना टूटा हुआ देखा था. अंसारी के टूट जाने ने सभी मज़दूरों की उन झूठी उम्मीदों को तोड़ दिया था जिसकी डोर से बंधे वे रोज़ पिछले सात सालों से बिला नागा मिल की ज़मीन पर मत्था टेकते थे.
``अंसारी साहब की मिल 52 बीघे में फैली है और उसकी कीमत एक अरब रुपये से ऊपर है. सरकार ने पिछले सात सालों से उनकी मिल बंद करा दी है और अब बताओ एक उद्योगपति को यह मिल सिर्फ पांच करोड़ रुपये में बेची जा रही है. दस करोड़ का तो अंसारी साहब पर कर्जा हो गया है. क्या होगा उनका और क्या होगा मज़दूरों का....उनके परिवारों का....´´ पिताजी बहुत परेशान थे. वे बहुत भोले थे, उन्हें अपने परिवार से ज़्यादा मज़दूरों की चिंता थी. वे इस बात को मान ही नहीं सकते थे कि वे भी एक अदने से मज़दूर हैं. मैंने सोचा कि अगर किसी अच्छे अखबार में नौकरी मिल जाती तो हमारी बहुत सी समस्याएं हल हो सकती थीं लेकिन अच्छे अखबार में नौकरी के लिये किसी अच्छे आदमी से परिचय होना ज़रूरी था और सभी अच्छे आदमी राजनीति में चले गये थे.
उदभ्रांत के लिये देखे गये हमारे सपने भी टूटते दिखायी दे रहे थे. उसने बी.एस सी. करने के बाद हमारी मर्ज़ी के खिलाफ एम.एस सी छोड़कर समाजशास्त्र से एम.ए. करने का विकल्प चुना था और अब जो रास्ते थे मुझसे ही होकर जाते थे. अपना अधिकतर समय वह बाबा के साथ बिताया करता था और बाबा की सोहबत की वजह से उसे अजीब-अजीब किताबें पढ़ने का चस्का लग चुका था. मैंने अपनी कविताई के शुरुआती दिनों में जो किताबें बटोरी थीं उनमें मुक्तिबोध और धूमिल जैसे कवियों की भी किताबें थीं. वह पता नहीं कब मेरी सारी लाइब्रेरी चाट चुका था और आजकल अजीब मोटी-मोटी किताबें पढ़ता था जिनमें से ज़्यादातर को पढ़ने की कोशिश करने पर पिताजी को सिर्फ प्रगति प्रकाशन, मास्को ही समझ में आता था. मैंने कभी उसकी किताबें पढ़ने की कोशिश नहीं की थी. अव्वल तो मेरे पास समय नहीं था और दूसरे मैं पिताजी जितना चिंतित भी नहीं था. आखिर घिसट कर ही सही, घर का ख़र्च जैसे-तैसे चल ही रहा है और फिर जो भी हो, उदभ्रांत का मन आखिर पढ़ाई में ही तो लग रहा है, साइंस न सही आर्ट्स ही सही. एक बार तो उसने मुझे भी कहा कि मैं एम. ए. की पढ़ाई के लिये प्राइवेट ही सही फॉर्म भर दूं. मैंने मुस्करा कर मना कर दिया और उससे कहा कि मेरे जो सपने हैं उससे ही होकर गुज़रते हैं.
हमारे पूरे शहर को नीली झंडियों, नीली झालरों और नीले बैनरों से पाटा जा रहा था. हम जिधर जाते उधर मुस्कराता हुआ नीला रंग दिखायी देता. पोस्टरों में नीले रंग की उपलब्धियां गिनायी गयी थीं कि नीले रंग की वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियां बन गयीं, नीले रंग की वजह से कितने घरों के चूल्हे जलते हैं और इस महान नीले रंग ने कितने बेघरों को घर और बेसहारों को सहारा दिया है. इस नीले रंग का जन्मदिन आने वाला था और यह एक बहुत शान का मौका था, हालांकि कुछ अच्छे लोगों ने कहा कि यह पैसे की बर्बादी और झूठा दिखावा है.
पिताजी के साथ सात साल से बराबर धरने पर बैठने वाले मज़दूरों को धरने की आदत पड़ गयी थी. उनमें से कुछ जो चतुर थे उन्होंने अपने लिये दूसरी नौकरियां खोज ली थीं लेकिन ज़्यादातर मज़दूर आशावादी थे और उन्हें लगता था कि वे जब किसी सुबह सो कर उठेंगे तो मिल खुल चुकी होगी और उनका पिछले सालों का वेतन जोड़ कर दिया जायेगा. उनके पास एक साथ ढेर सारे पैसे हो जाएंगे और जिं़दगी बहुत आराम से चलने लगेगी. उनका सोचना ऐसा ही था जैसा मैं और उदभ्रांत ज़मीन पर नक्शा बना कर अपने-अपने कमरों की कल्पना करते थे जिसे न बनना था न बना. जिस दौरान पूरा शहर दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था, पिताजी और उनके साथ के मज़दूरों ने एक योजना बनायी. उनका मानना था कि राज्य का जो सबसे बड़ा हाकिम है उसके पास अपना दुखड़ा लेकर जायेंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि आखिर उनके परिवार वालों की भुखमरी का ज़िम्मेदार कौन है. हाकिम को हाथी की सवारी बहुत पसंद थी. उसका हाथी बहुत शांत था और कभी किसी पर सूंढ़ नहीं उठाता था. हाथी के बारे में कोई भी बात जानने से पहले संक्षेप में उसका यह इतिहास जानना ज़रूरी है कि उसे लम्बे समय तक राजाओं ने अपने पंडित पुरोहितों की मदद से ज़बरदस्ती पालतू बना कर रखा था और उस पर खूब सितम ढाये थे. बाद में एक ऐतिहासिक आंदोलन के ज़रिये हाथी को अपने वजूद का एहसास हुआ. उम्मीदें जगीं कि अब इस आंदोलन से जिन्हें पीछे धकेल दिया गया है, उन्हें आगे आने में मदद मिलेगी. सबने हाथी की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देखा. जब हाथी को अपनी ताकत का एहसास होना शुरू हुआ और इसने अपने लूट लिये गये वजूद को वापस पाने की कोशिशें शुरू की ही थीं कि हाकिम जैसे लोग इस पर सवार होने लगे और अब हाथी की सारी सजावट और हरकतें हाकिम की कोशिशों का नतीजा थीं. हाथी अब अपनी सजावट के बाहर आने के लिये तड़फड़ाता रहता था और हाकिम की कोशिश यही थी कि हाथी अपने फालतू अतीत को सिर्फ़ तभी याद करे जब उसे लोगों की संवेदनाएं जगा कर उनसे कहीं मुहर लगवानी हो या कोई बटन दबवाना हो. पिताजी जैसे लोगों की सारी उम्मीदें हाथी से जुड़ी थीं लेकिन हाकिमों की वजह से लगता था कि सब बेमानी होता जा रहा है. हाथी के दो दांत बाहर थे और वे काफी ख़ूबसूरत थे. वे पत्थर के दांत थे और किसी जौहरी से पूछा जाता तो वह शर्तिया बताता कि ये इतने महंगे पत्थर थे कि इतने में कई अस्पताल या स्कूल बनवाये जा सकते थे या फिर कई गांवों को कई दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था.
अंदर के दांतों का प्रयोग खाने के लिये किया जाता था और हाथी को खाने में हर वह चीज़ पसंद थी जो रुपयों से ख़रीदी जा सकती थी. हाथी को उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था जो सीधे-सीधे दिखायी नहीं देती थीं जैसे संवेदनाएं, भावनाएं, मजबूरियां, टूटना और ख़त्म होना आदि आदि. हाथी बहुत ताक़तवर था और उसे यह बात पता थी इसीलिये वह कभी किसी के सामने सूंढ़ नहीं उठाता था. वह विनम्र कहलाया जाना पसंद करता था और उसे अपनी अनुशासनप्रिय छवि की बहुत परवाह थी. हाथी की पीठ पर विकास का हौदा रखा रहता था जो हमेशा ख़ाली रहता था लेकिन हाथी उसके बोझ तले ख़ुद को हमेशा दबा हुआ दिखाना पसंद करता था. हाथी कभी-कभी मज़ाक के मूड में भी रहता था. जब वह अच्छे मूड में होता तो उस दिन महावत को यह चिंता नहीं हुआ करती थी कि हाथी कभी भी उसे नीचे पटक सकता है. हाथी के महावत बदलते रहते थे और महावतों की जान हमेशा पत्ते पर रहती थी क्योंकि वह जानते थे कि हाथी उन्हें सिर्फ़ अच्छे मूड में ही पीठ पर बिठाता है वरना उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह हाथी की पूंछ भी छू सकें. हाथी को जनता के पैसे से लाया गया था और उसका भोजन और ज़रूरत की अन्य चीज़ें भी जनता के धन से आती थीं लेकिन यह बात हाथी को पता नहीं थी. उसे शायद यह बताया गया था कि इस धन पर उसका और सिर्फ़ उसका ही हक़ है. वह अपने भविष्य के लिये अच्छी बचत कर रहा था और इसके दौरान वह अपनी ख्याति को लेकर भी बहुत चिंतित रहता था. इसके लिये वह कुछ भी करता रहता था और इस दौरान कई बार मज़ाकिया मूड में होने पर वह न्याय के लिये बनायी गयी संस्थाओं का भी उपहास करने से नहीं चूकता था.
मैंने एक अख़बार में चुपके से बात की थी और एक अच्छे अख़बार से मुझे आश्वासन भी मिला था. मैं जब नीलू के घर पहुंचा तो आंटी ने मेरी ओर बहुत टेढ़ी नज़रों से देखा. मैं चुपचाप थके कदमों से ऊपर पहुंचा तो नीलू आसमान की ओर नहीं देख रही थी. उसकी आंखों में ख़ालीपन था और उसकी शलवार कमीज़ नीली थी. मैंने आसमान की ओर नहीं देखा. मैं पता नहीं क्यों कुछ सहमा और ख़ाली सा महसूस कर रहा था, बिल्कुल नीलू की आंखों की तरह. वह ख़ामोशी वहां मौजूद हवा में घुल रही थी और हवा भी उदास हो रही थी. वह छत पर लगे सेट टॉप बॉक्स की ओर एकटक देखे जा रही थी और मुझे याद आया कि मेरे घर में सेट टॉप बॉक्स नहीं है. मेरे घर में न ही फ्रिज है, न ही वाशिंग मशीन और मैं किराये के घर में रहता हूं. मैं जानता हूं इन बातों का इस समय कोई मतलब नहीं है और मुझे तुरंत जाकर नीलू की उदासी का कारण जानने की कोशिश करनी चाहिये लेकिन मेरी हर उदास तुलना तभी होती है जब कोई उदास लम्हा मेरी ज़िंदगी में आ कर इसे और दुश्वार बनाने वाला होता है. मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि जो सवाल मेरे मन में नीलू के घर को देख कर उठ रहे हैं, वे कुछ देर में मेरे सामने आने वाले हैं. नीलू ने मुझे तब तक नहीं देखा जब तक मैं उसके एकदम क़रीब जाकर खड़ा नहीं हो गया.
``अरे साहब....कब आये ?´´ उसकी आवाज़ में जो टूटन थी वह मैंने पिछले कुछ समय में पिताजी की आवाज़ में छोड़ कर दुनिया में और किसी की आवाज़ में नहीं महसूस की थी. उसका साहब कहना मेरे लिये ऐसा था कि मैंने ताजमहल बनाया है और मुझे सबके सामने उसके निर्माता के रूप में पुकारा जा रहा है. मगर उसकी आवाज़ टूटी और बिखरी हुयी थी और उसके टुकड़े इतने नुकीले रूप में बाहर आ रहे थे कि मुझे चुभ रहे थे. एक टुकड़ा तो मेरी आंखों में आ कर ऐसा चुभा कि मेरी आंखों में पानी तक आ गया. मेरी धड़कन धीरे-धीरे डूबती जा रही थी और लग रहा था मैं देर तक खड़ा नहीं रह पाउंगा. उसने मेरी तनख़्वाह पूछी और उदास हो गयी. मैंने आसमान का रंग देखा और उदास हो गया. चांद ने हम दोनों के चेहरे देखे और उदास हो गया.
लड़के ने नीलू को देखकर हां कह दी थी और दो परिवारों के महान मिलन की तैयारियां होने लगी थीं. नीलू ने मेरी तनख़्वाह पूछी थी और भरे गले से मुझसे कहा था कि तुम 2010 में 1990 की तनख्वाह पर कब तक काम करते रहोगे और अपनी उंगलियां बजाने लगी थी. मैंने उससे कहा कि बजाने से उंगलियों की गांठें मोटी हो जाती हैं. उसने कहा कि मैं कुछ भी कोशिश नहीं कर रहा हूं और एक भाग्यवादी इंसान हूं. मैंने उसे बताया कि एक बड़े अखबार में मेरी नौकरी की बात चल रही है और जल्दी ही मुझे पत्रिका के उन अनपढ़ अधेड़ों से छुटकारा मिल जायेगा. में नीलू के बगल में बैठा था और उसने धीरे से मेरी हथेली थाम ली.
``यह सच है ना साहब कि हमारे आने से पहले भी दुनिया इसी तरह चल रही थी.´´ उसकी आवाज़ की अजनबियत को पहचानने की कोशिश में मैंने सहमति में उसकी हथेलियां दबायीं.
``और हमारे जाने के बाद भी सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा ना ?´´ उसने पूछते हुये पहली बार आसमान को देखा. बादल थे या धुंए की चादर कि आसमान का रंग काला दिखायी दे रहा था और लगता था किसी भी पल कहीं भी भूकम्प आ सकता है.
``हां, शायद.´´
``मेरा दिल नहीं मानता साहब.´´
``क्या ?´´
``कि हमने अपने आसपास की दुनिया को इतना ख़ूबसूरत बनाया है, अपने हिस्से के आसमान को, ज़मीन को, हवा को, अपनी छोटी सी दुनिया को और हमारे सब कुछ ऐसे ही छोड़ कर चले जाने पर किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. कितनी स्वार्थी हवा है न हमारे आसपास ?´´
प्रश्न- मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, वह लड़की भी मुझसे प्यार करती है लेकिन हमारी हैसियत में बहुत फर्क है. मैं बहुत गरीब घर से हूं और वह अमीर है. मैं उसके बिना नहीं जी सकता लेकिन उसके घर वाले हमारी शादी को कभी राज़ी नहीं होंगे. मैं क्या करुं ?
उत्तर-आप दोनों भले ही एक दूसरे से प्यार करते हों, शादी एक बहुत बड़ा निर्णय होता है. आपको अपने संसाधन देखने होंगे कि क्या आप शादी के बाद अपनी पत्नी के सारे खर्चे आसानी से उठा सकेंगे. आप उसको दुखी नहीं कर सकते जिससे प्रेम करते हों. आपको अपने परिवार के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, सिर्फ़ अपनी खुशी के बारे में सोच कर स्वार्थी नहीं बना जा सकता.
मैं चुप रहा. मेरे पास नीलू से कहने के लिये कुछ नहीं था, कुछ बची हुयी मज़बूत कविताएं और एक बची हुयी कमज़ोर उम्र थी मेरे पास जो उसे मैं नहीं देना चाहता था. वह निश्चित रूप से इससे ज़्यादा की हक़दार थी, बहुत ज़्यादा की. मेरी बांहें बहुत छोटी थीं और तक़दीर बहुत ख़राब, मैं उन्हें जितना भी फैलाऊं, बहुत कम समेट पाता था.
मैंने पूछा कि क्या शादी की तारीख पक्की कर ली गयी है तो उसने कहा कि अगर दुनिया के सारे लोग एक के ऊपर एक खड़े कर दिये जायें तो भी चांद पर नहीं पहुंच सकते. चांद बहुत दूर है. मैंने उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछा और उसने मेरे परिवार के बारे में. हमने चार बातें कीं, तीन बार एक दूसरे की हथेलियां सहलायीं, दो बार रोये और एक बार हंसे. उसके थरथराते होंठ मैंने एक बार भी नहीं चूमे, शायद यही वह पाप था जिसके कारण नीचे उतरते ही मेरा बुरा समय शुरू हो गया. मैं चाहता था कि सबकी नज़रें बचा कर निकल जाऊं. अंकल हॉल में अखबार पढ़ रहे थे और आंटी बैठ कर स्वेटर बुन रही थीं. दोनों ही ऐसे काम कर रहे थे जो आमतौर पर रात में नहीं किये जाते और मैं समझ गया था कि आज मुझे नीलू की आंखों के साथ उसके होंठ भी चूमने चाहिये थे. उसके होंठों के आमंत्रण और और आंखों के निमंत्रण को मैंने जान-बूझ कर नज़रअंदाज़ किया था क्योंकि उस वक़्त मैं नीलू को इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं पहुंचा सकता था. उसकी उपेक्षा करने का मेरे पास यही तरीका था. मेरे मन में कहीं किसी मतलबी और नीच जानवर ने धीमे से कहा था कि नीलू ने शादी से मना क्यों नहीं किया...गेंद तुम्हारे पाले में क्यों..? क्या तुम्हारी सामाजिक स्थिति उसके लिये भी....?
``हद्दी यहां आना.´´ अंकल के बुलाने के अंदाज़ से ही लग गया कि आवाज़ उनकी थी लेकिन वह जो बात कहने जा रहे थे उसकी भाषा और रणनीति आंटी की थी. मेरे नाम को अंकल और उन जैसे मुहल्ले के कई लोगों ने ख़राब कर दिया था और वे कभी मुझे मेरे असली नाम से नहीं पुकारते थे. क्या फ़ायदा ऐसे नाम रखने का कि हम उस पर दावा भी न दिखा पाएं. मैं तो चुपचाप सुन लेता था लेकिन उदभ्रांत अपना नाम बिगाड़ने वालों से उलझ जाता था.
``देखो बेटा, नीलू की सगाई तय हो गयी है. तुम उसके सबसे क़रीबी दोस्त हो, उसे समझाओ कि शादी के लिये मना न करे, मन बनाये. अरे शादी कोई कैरियर बनाने में बाधा थोड़े ही है. तुम्हारी बात वह समझेगी, उसे समझाओ. उसे तैयार करने की ज़िम्मेदारी तुम्हारी है और हां बाजार से कुछ चीज़ें भी लानी होंगी. तुम तो ऑफिस में रहते हो, कल दिन में उद्दी को भेज देना तुम्हारी आंटी की थोड़ी मदद कर देगा....तुम तो जानते ही हो कि मुझे ऑफिस से छुट्टी मिलना कितना......´´ अंकल काफ़ी देर तक बोलते रहे और मैं खड़ा टीवी को देखता रहा. टीवी में बताया जा रहा था कि शहर की सजावट में कितने करोड़ रुपये खर्च हुये हैं और नीला रंग शहर के लिये कितना ज़रुरी है. अंकल की बातें बहुत चुभ रही थीं इसलिये मैंने टीवी की ओर नज़रें कर ली थीं. टीवी पर जो बताया जा रहा था वह भी इतना चुभ रहा था कि मैं उनकी बातें अधूरी छोड़ कर निकल आया.
प्रश्न- मैं एक पिछड़े परिवार से संबंध रखता हूं. मेरे पिताजी एक जगह चपरासी का काम करते हैं और मां घरों के बरतन मांजती है. मेरी पढ़ाई का खर्च वे बड़ी मुश्किल से उठा पा रहे हैं लेकिन आजकल मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता. मेरे मुहल्ले के लोग मेरी उपलब्धियों को भी मेरी जाति से जोड़ कर देखते हैं और कुछ भी करने का मेरा उत्साह एकदम ख़त्म होता जा रहा है. मेरे मुहल्ले के लोग मेरा नाम तक बिगाड़ कर बुलाते हैं. मैं सोचता हूं कोई संगठन ज्वाइन कर लूं. मेरे सामने ही मेरे पिता की बेइज़्ज़ती की जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं क्या करूं ?
उत्तर- आप चाहें तो किसी संगठन में शामिल हो सकते हैं लेकिन ये आपकी परेशानियों को कम नहीं करेगा. आपके पिताजी का अपमान करने वाले लोग संख्या में बहुत ज़्यादा हैं और किसी संगठन से उनका जवाब देने की आपकी उम्र भी नहीं है. आपके पास एकमात्र हथियार आपकी पढ़ाई है. खूब पढ़िये और किसी अच्छी जगह पर पहुंचिये फिर आपका मज़ाक उड़ाने वाले लोग ही आपसे दोस्ती करने को बेकरार दिखायी देंगे. अपने गुस्से को पालिये और उसे गला कर उसे एक नुकीले हथियार के रूप में ढाल दीजिये.
उदभ्रांत ने मुझसे पूछा कि क्या मैं नीलू को पसंद नहीं करता. मैंने कहा कि नीलू मेरी अच्छी दोस्त है तो वह बहुत ज़ोर से हंसा. उसने मुझसे ऐसी भाषा में बात की जैसे पहले कभी नहीं की थी. उसने मुझसे पूछा कि क्या उसका हाथ मुझे अपने हाथ में लेते हुये कभी लगा कि दुनिया को उसके हाथ की तरह गरम और सुंदर होना चाहिये. मैंने उसे बताया कि ऐसा मुझे हर बार लगा है जब मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया है और फिर उसे समझाया कि नीलू मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ और अच्छी दोस्त है और मेरी दिली इच्छा है कि उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो. उसने कहा कि मुझे फिर से कविताएं लिखना शुरू कर देना चाहिये क्योंकि अगर मरना ही है तो कविताएं लिखते हुये मरने से अच्छा काम कोई नहीं हो सकता. मैंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई पेट है और उसने कहा कि कुछ सोच कर पेट को दिमाग और दिल के नीचे जगह ही गयी है. मैंने निराश आवाज़ में उससे कहा कि इस दुनिया में हमारे जीने के लिये कुछ नहीं है तो उसने कहा कि हमारे पास धार है तलवार भले ही न हो. मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कॉलेज जाने के लिये सायकिल चाहिये. उसने कहा कि न तो उसे कॉलेज जाने के लिये सायकिल की ज़रूरत है और न ही नौकरी पाने के लिये हाथी की. मुझे यह अजीबोग़रीब तुलना समझ में बिल्कुल नहीं आयी और मुझे भी पिताजी की बात पर विश्वास होने लगा कि उदभ्रांत आजकल कोई नशा करने लगा है. मैंने कहा कि सायकिल से हाथी की क्या तुलना, यह तुलना बेकार है.
उसने लॉर्ड एक्टन नाम के अपने किसी टीचर का नाम लेते हुये कुछ बातें कीं और कहा कि मैं भोला हूं जो सामने दिखायी दे रही चीज़ पर तात्कालिक फैसला दे रहा हूं जबकि न तो सायकिल और हाथी में कोई फर्क होता है और न ही दुनिया के किसी भी फूल और शरीर के किसी भी अंग में. मुख्य बात तो वह सड़क होती है जिधर से वह सायकिल या हाथी निकलते हैं. सड़क मजेदार हो तो जितना खतरनाक झूमता हुआ हाथी होता है, सायकिल उससे रत्ती भर कम ख़तरनारक नहीं. मैंने उससे कहा कि तुम हाथी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हो तुम्हें पता नहीं इसका परिणाम क्या हो सकता है, हो सकता है हाथी इधर ही कहीं टहल रहा हो. वह मुस्कराने लगा. उसने बांयीं आंख दबा कर बताया कि हाथी आजकल शहर में नहीं है, वह खेतों की तरफ निकल गया है. मैंने आश्चर्य व्यक्त किया, ``क्यों खेतों की ओर क्यों ?´´
``दरअसल हमें एक ऐसी चीज़ किताबों में पढ़ाई जाती रही है जिसे पढ़ना एकदम अच्छा नहीं लगता. `भारत गांवों का देश है´ या `भारत एक कृषिप्रधान देश है´ जैसी पंक्तियां पढ़ने से हमारे देश की गरीबी और बदहाली का पता चलता है. खेत और किसान बहुत बेकार की चीज़ें हैं और ये हमेशा बहुत गंदे भी रहते हैं जिससे सौंदर्यबोध को धक्का लगता है. इसलिये कुछ ऐसे लोगों ने, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं और जो देश को ऊंची-ऊंची इमारतों और चमचमाते बाज़ारों से भर कर इसे एकदम चकाचक बना देना चाहते हैं, हाथी से अपने देश की गरीबी दूर करने की प्रार्थना की है. हाथी सजधज कर, अपने दांतों को हीरे पन्नों से सजा कर और इन दयालु लोगों का दिया हुआ मोतियों जड़ा जाजिम पहन कर खेतों की ओर निकल गया है. वह जिन-जिन खेतों से होकर गुज़रेगा, उन खेतों की किस्मत बदल जायेगी. वहां खेती जैसा पिछड़ा हुआ काम रोक कर बड़ी-बड़ी इमारतें, चमचमाती सड़कें बनायी जायेंगीं. जिस पर से होकर बड़े-बड़े दयालु लोगों की बड़ी-बड़ी गाड़ियां गुज़रेंगीं.´´
मैं समझ गया कि उदभ्रांत का दिमाग, जैसा कि पिताजी पिछले काफी समय से कह रहे थे, ज़्यादा किताबें पढ़ने से और ख़राब संगत में रह कर नशा करने से सनक गया है.
``तुम आजकल रहते कहां हो और रात-रात भर गायब रहते हो....किन लोगों के साथ हो और क्या कर रहे हो पढ़ने लिखने की उम्र में ?´´ मैंने उसे ताना देकर उसे वापस सामान्य करना चाहा. वह ज़ोर से हंसने लगा और एक कविता पढ़ने लगा जिसमें किसी की आंखों को वह दर्द का समंदर बता रहा था.
मैंने उससे धीरे से कहा कि उसे इस उम्र में कविताएं नहीं पढ़नी चाहियें, उसने कहा कि इस उम्र में कविताओं का जो नशा है उसके सामने दुनिया को कोई नशा ठहर नहीं सकता. उसने उठते हुये मुझसे कहा कि मुझे नीलू को कोर्ट में ले जाकर शादी कर लेनी चाहिये क्योंकि आसमान तक सीढ़ी लगाने के लिये एक मर्दाना और एक जनाना हाथ की ज़रूरत होती है.
पिताजी बड़े अरमानों से अपने साथ कुछ पढ़े-लिखे और समझदार माने जाने वाले मज़दूरों को लेकर निकले थे और अधिकतर मज़दूरों का मानना था कि राज्य के सबसे बड़े हाकिम के पास जाने से उनकी समस्या तुरंत हल हो जायेगी क्योंकि शायद उनको पता ही न हो कि उनके अपने लोग कितनी मुसीबतों में घिरे हैं. वे लोग अपने हाथों में निवेदन करती हुयी कुछ तख्तियां लिये हुये थे जिसमें चीत्कार करती हुयी पंक्तियां लिखी थीं जो वहां के पढ़े-लिखे मज़दूरों ने बनायी थीं और कुछ तिख्तयों पर तो उदभ्रांत ने कुछ कविताएं भी लिखी थीं. पिताजी लम्बे समय के अंतराल के बाद उदभ्रांत के किसी काम पर ख़ुश हुये थे.
वे लोग जब एक गली से होते हुये मुख्य सड़क पर पहुंचे तो वहां पहले से एक राजनीतिक पार्टी के कुछ लोग तख्तियां लिये हुये नारे लगाते हुये जा रहे थे. उन लोगों ने लाल टोपियां पहन रखी थीं और उन लोगों को रिकॉर्ड करते हुये कुछ टीवी वाले लोग भी थे. जिधर वे टीवी वाले लोग अपना कैमरा घुमाते उधर के लोगों में जोश आ जाता और वे चिल्ला-चिल्ला कर नारे लगाने लगते. पिताजी ने उन लोगों से दूरी बनाये रखी. जब वे लोग मुख्य सड़क पर आये तो वहां पुलिस की तगड़ी व्यवस्था थी. कई मज़दूरों के हाथ-पांव फूल गये और कई मज़दूर जोश में आ गये. पिताजी ने सभी मज़दूरों को समझाया कि कोई अशोभनीय बात और हिंसात्मक हरकत उनकी तरफ से नहीं होनी चाहिये लेकिन एकाध मज़दूरों का कहना था कि आज वे अपने सवाल पूछ कर जायेंगे और किसी से नहीं दबेंगे. पुलिस का एक बड़ा अफ़सर पिताजी के पास आया और उसने बड़ी शराफ़त से पिताजी से पूछा कि उनकी समस्या क्या है. पिताजी ने कहा कि उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं. फिर वह अफसर उस पार्टी के प्रमुख के पास गया, उसने भी कहा कि हमें भी कुछ सवाल पूछने हैं. दोनों लोगों से बात करने के बाद अफ़सर थोड़ा पीछे हटा और भाषण देने वाली मुद्रा में हाथ उठा कर दोनों तरफ के लोगों को शांति से अपने-अपने ठिकानों पर लौट जाने की सलाह दी. उसका कहना था कि उनके सवालों के जवाब एक-दो दिन में कूरियर से उनके घर भिजवा दिये जाएंगे या फिर किसी अख़बार में अगले हफ्ते उनके उत्तर छपवा दिये जायेंगे. दोनों तरफ के लोग खड़े रहे. अफ़सर ने फिर अपील की कि सभी लोग यहीं से लौट जायें और उसे लाठीचार्ज करने पर मजबूर न करें. उसके एक मातहत ने आकर उसके कान में धीरे से कहा कि लाठीचार्ज और गोली चलाने जैसी घटना से उन्हें बचाना चाहिये क्योंकि इससे बहुत पैसे खर्च कर साफ करवायी हुयी सड़क पर खू़न के धब्बे लग सकते हैं जो हाथी को कतई पसंद नहीं आयेंगे. अफ़सर मुस्कराया और बोला कि बेवकूफ तू इसीलिये मातहत है और मैं अफ़सर, अगर ये लोग नहीं भागे तो इन पर ऐसी लाठियां बरसायी जायेंगी कि एक बूंद ख़ून भी नहीं गिरेगा और ये कभी उठ नहीं पायेंगे, उसने आगे यह भी जोड़ा कि राजनीतिक पार्टी के इन लोगों पर लाठियां बरसाने से उसे अपनी छवि चमकाने का भी मौका मिलेगा और पदोन्नति की संभावनाएं बढ़ जायेंगीं. पिताजी और उनके साथ के मज़दूर वहीं ज़मीन पर बैठ गये. पिताजी का कहना था कि वे शांतिपूर्ण ढंग से वहां तब तक बैठे रहेंगे जब तक उनके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते.
इधर उस पार्टी के लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि पुलिस लाठी चलाना शुरू क्यों नहीं कर रही है. आखिरकार एक युवा कार्यकर्ता, जो खासतौर पर लाठी खाने अपने एक फोटोग्राफर दोस्त को लेकर आया था, ने चिंताग्रस्त होकर पुलिस टीम की तरफ एक बड़ा पत्थर उछाल दिया. पत्थर एक हवलदार की आंख पर लगा और उसकी आंख फूट गयी. उसने एक आंख से पार्टी के लोगों की तरफ देखा और उसे अहसास हुआ कि `लाठीचार्ज´ या `फायर´ बोल पाने की ताकत रखना कितनी बड़ी बात होती है. तब तक दूसरा पत्थर आया. ये किसी और चिंतित कार्यकर्ता ने फेंका था. पुलिस टीम के ऊपर एक के बाद चार-पांच पत्थर पड़े तो अफ़सर को लाठीचार्ज का आदेश देना पड़ा.
भगदड़ मच गयी और भागते हुये लोग पिताजी और उनके लोगों के ऊपर गिरने लगे क्योंकि ये लोग बैठे हुये थे. ये जब भी उठने की कोशिश करते, कोई इन्हें धक्का देकर भाग जाता. पुलिस टीम राजनीतिक पार्टी के लोगों को दौड़ाती हुयी पिताजी के पास आयी और जो मिला उस पर लाठियों के करारे प्रहार करने शुरू कर दिये. सड़क पर वाकई एक बूंद भी खून नहीं गिरा और पूरी सजावट ज्यों की त्यों चमकदार बनी रही. पत्रकारों और कैमरा वालों ने हड्डी टूटे हुये लोगों की कुछ तस्वीरें खींचीं और फिर सड़क पर लगी तेज़ नियॉन लाइटों वाली ग्लोसाइन के चित्र लेने लगे जिसमें जल्दी ही एक ख़ास अवसर पर गरीबों के लिये ढेर सारी योजनाओं की घोषणा किये जाने की घोषणा की गयी थी.
पिताजी भी उन तीन गंभीर रूप से घायल लोगों में से थे जिनकी हडि्डयां टूटी थीं और उन्हें तब तक चैन नहीं आया जब तक कि डॉक्टर ने यह कह कर उन्हें निश्चिन्त नहीं कर दिया कि उनके दो साथियों की तरह उनकी भी दो-तीन हडि्डयां टूटी हैं. वह निश्चिन्त हुये कि उन्होंने अपने साथियों से धोखा नहीं किया. पिताजी के कई मित्र अस्पताल में उनका हाल-चाल पूछने आये और अंसारी साहब भी आकर उनका पुरसाहाल कर गये. एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर भी आया और देर तक पिताजी के पास बैठा कुछ लिखता रहा. उसने पिताजी से उनका अगला-पिछला पूरा रिकॉर्ड पूछा, घर-परिवार, बीवी-बच्चे, खान-पान सबके बारे में पूछा और जाते वक़्त सलाह दी कि उन्हें सरकार का विरोध करने जैसा देशद्रोह वाला काम नहीं करना चाहिये. पिताजी ने नज़रें दूसरी ओर फेर लीं जिस पर उसने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ तो ज़िम्मेदार आप होंगे.
`उत्तर प्रदेश´ में सवालों के जवाब नहीं दिये जाते
पिताजी बारह दिनों बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आ गये थे और प्लास्टर लगवा कर पूरी तरह से बेडरेस्ट में थे. किसी सुबह वह बहुत मूड में दिखायी देते और हम दोनों भाइयों को बुला कर मिल से संबंधित पुरानी कहानियां सुनाते. जब मां खाना बना लेती तो खाना परोसे जाने से पहले मां को भी अपने पास बुलाते और अपनी शादी के दिनों का कोई किस्सा छेड़ देते जिससे हम हंसने लगते और मां थोड़ी शरमा जाती. ऐसे ही एक अच्छे दिन उन्होंने अख़बार पढ़ते हुये हम लोगों को सुनाते हुये कहा कि अगले हफ्ते एक बहुत अच्छी फिल्म आने वाली है उसे दिखाने ले चलेंगे और उसके टैक्स फ्री होने का इंतज़ार नहीं करेंगे. मां ने पूछा कि कैसे मालूम कि फि़ल्म अच्छी है तो उन्होंने कहा कि जिस फिल्म का नाम ही `डांस पे चांस´ हो वो तो अच्छी होगी ही. मां ने कहा कि वे नये अभिनेताओं-अभिनेत्रियों को नहीं पहचानतीं इसलिये उन्हें मज़ा नहीं आयेगा. पिताजी ने कहा कि अगर वे नखरे करेंगी तो वे उन्हें उठा कर ले जायेंगे. ये कहने के बाद पिताजी बेतरह निराश हो गये और अखबार में कोई सरकारी विज्ञापन पढ़ने लगे. जिस दिन वह उदास रहते दिन भर किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते. मिल और मज़दूरों को लेकर कुछ बड़बड़ाते रहते और चिंता करते रहते. ऐसे ही एक उदास दिन उन्होंने कहा कि उनके न रहने पर भी इस घर पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि उनके दो जवान बेटे सब कुछ अच्छे से संभाल सकते हैं. मां साड़ी का पल्लू मुंह में डाल कर रोने लगीं तो उन्होंने कहा कि मैंने दो शेर पैदा किये हैं और इनके रहते तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे दोनों बेटे मेरे जैसे ही बहादुर हैं. ये कहने के बाद वह बुरी तरह अवसाद में चले गये और अख़बार में साप्ताहिक राशिफल पढ़ने लगे. मैं अक्सर घर के माहौल से तंग आ जाता था और छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस पहुंच जाता था मगर वहां और भी ज़्यादा घुटन थी.
मैं ऑफिस के लोगों की बद्तमीज़ियों से बहुत तंग आ गया था. बॉस के आकर उजड्डई करने के बाद मैं अब शिकायत भी किससे करता. मैं जब उस दिन ऑफिस में घुसा तो एक साथ दादा और दीन जी दोनों ने अपनी बद्तमीज़ियां शुरू कर दीं. दीन जी का सवाल बहुत ही घिनौना था तो दादा का सवाल यह था कि उन्होंने अपनी रिश्ते की एक बहन से सेक्स करने की अपनी इच्छा के बारे में मुझसे सलाह मांगी थी. मेरा दिमाग भन्ना गया. वे मेरे बिना पूछे ही बताने लगे कि दुनिया में इस तरह के संबंधों का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग अपनी कुंठाएं बिना झिझक बाहर निकाल रहे हैं. उन्होंने मुझे और दादा को इस तरह के संबंधों पर आश्चर्य व्यक्त करने पर लताड़ा और इस तरह के संबंधों का नाम इनसेस्ट सेक्स बताया और यह भी बताया कि अब यह बहुत तेज़ी से हर जगह फैल रहा है और सहज स्वीकार्य है. दादा इस पर सहमत नहीं हुये और कहा कि परिवार में ऐसे संबंध उचित नहीं हैं, हां आपस में दो परिवार बदल कर ये करें तो चल सकता है. पिताजी के पांव और कोहनी का फ्रैक्चर मुझे अपने ऑफिस में भी अलग-अलग लोगों के अलग-अलग अंगों में दिखायी दे रहा था. उस दिन मैं लंच करने नहीं गया और दादा मुझे दो बार पूछने के बाद हंसते हुये चले गये. जब सभी लोग लंच करने चले गये तो मैंने दादा की दराज से एक मोटा स्केच पेन निकाला.
वापस आने के बाद मेरी उम्मीदों के विपरीत वे लोग हंसने लगे. मुझे सीरियस लेना उन्हें अपमान की तरह लग रहा होगा, इस बात से मैं वाकिफ़ था. दादा अंदर बॉस के केबिन में गये और थोड़ी ही देर में मुझे क्रांतिकारी की तरफ से बुलावा आ गया.
``जी...सर.´´ मैं अंदर जा कर चपरासी वाले भाव से खड़ा हो गया.
``क्या हुआ भई, कोई दिक्कत..?´´ उसने हंसते हुये पूछा. उसके एक तरफ दादा और दूसरी तरह `दीन´ खड़े थे.
``जी....कोई ख़ास नहीं.´´ मैंने बात को समेटने की कोशिश की.
``सुना है तुमने अपनी खिड़की पर लिख दिया है कि `उत्तर प्रदेश में सवालों के जवाब नहीं दिये जाते´ ?´´ उनकी मुस्कराहट बदस्तूर जारी थी.
``जी नहीं...मैंने सिर्फ़ यह लिखा है कि `जवाब नहीं दिये जाते´, उत्तर प्रदेश तो पहले से मौजूद था.´´
इस पर वे तीनों लोग हंसने लगे. उनकी सामूहिक हंसी मेरा सामूहिक मानसिक बलात्कार कर रही थी पर वे अपनी जगह बिल्कुल सही थे क्योंकि वे मुझे तनख्वाह देते थे और इस लिहाज़ से मुझे ज़िंदा रखने के बायस थे.
``भई उत्तर प्रदेश में मत देना सवालों के जवाब, हम तुम्हें यहां बुला लिया करेंगे जब भी हमें उत्तर चाहिये होंगे....क्यों दादा ठीक है न ?´´ दादा ने भी हंसते हुये सहमति जतायी और देखते ही देखते प्रस्ताव 100 प्रतिशत वोटिंग के साथ पारित हो गया.
मैं मन मार कर कूद कर आया और अपनी कुर्सी पर आ कर बैठ गया. मेरा मन काम में कतई नहीं लग रहा था. तभी चपरासी ने खिड़की पर आकर सूचना दी कि कोई लड़की मुझसे मिलने आयी है. मैंने बिना कुछ सोचे समझे बाहर जाने का विकल्प चुना क्योंकि मुझसे किसी लड़की का मिलने आना इस घिनौने ऑफि़स के लिये एक और मसाला होता. मैं यह सोचता हुआ आया कि किसी कंपनी से कोई विज्ञापन वाली लड़की होगी लेकिन बाहर नीलू मिली.
``मेरे साथ थोड़ी देर के लिये बाहर चलोगे साहब ?´´ उसके प्रश्न में आदेश अधिक था सवाल कम. मैंने चपरासी को समझाया कि कोई मेरे बारे में पूछे तो वह कह दे कि खाना खाने गये हैं. पूरे ऑफि़स में चपरासी भग्गू ही मेरा विश्वासी था और ऑफि़स की जोकर पार्टी को कतई नहीं पसंद करता था.
नीलू मुझे ले कर शहर के एक प्रसिद्ध पार्क में पहुंची और वहां पहुंचते ही घास पर लेट गयी. शहर में पार्क और मूर्तियां बहुत थे लेकिन काम और रोटियां बहुत कम. उसने लाल रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी.
``आजकल घर नहीं आते साहब तुम ?´´ उसने मेरी ओर देखते हुये पूछा.
``तुम्हारी मम्मी ने मना किया है नीलू.´´ मैंने न चाहते हुये भी उसे सच बताया.
``अच्छा...बड़ा कहना मानते हो मेरी मम्मी का.´´ वह मुस्करायी तो मैं दूसरी ओर देखने लगा जहां एक जोड़ा एक दूसरे के साथ अठखेलियां रहा था.
``वह तुम्हारी भलाई चाहती हैं नीलू.´´ मैंने मरे हुये स्वर में कहा.
``मगर मैं अपनी बुराई चाहती हूं.´´ उसने नटखट आवाज़ में कहा. ``मुझे ज़िंदगी गणित की तरह नहीं जीनी साहब. मुझे जीना है अपने तरीके से जो बाद में अगर गलत साबित हुआ तो देखा जायेगा. उन्होंने मुझसे भी कहा कि प्यार से पेट नहीं भरता और मैं तुम्हें भूल जाऊं लेकिन आज मुझे लग रहा है कि प्यार से ज़रूर पेट भरता होगा तो लग रहा है बस्स.´´ मैं अपलक उसे देख रहा था. आज वह बहुत बदली सी लग रही थी.
``लाल में तुम थोड़ी ज़्यादा शोख़ लग रही हो....´´ मैंने उस पर भरपूर नज़र डाल कर कहा.
``तुम्हें क्या लगता है ?´´ उसने पूछा.
``किस बारे में....? लाल रंग भी तुम पर जंचता है लेकिन.....´´
``लाल रंग नहीं, प्यार के बारे में ? क्या प्यार से पेट भरता होगा ?´´ उसकी आवाज़ में सौ चिड़ियों की चहचहाहट थी और आंखों में हज़ार जुगनुओं की रोशनी.
``पता नहीं, मुझे नहीं लगता नीलू कि प्यार से.....´´ मेरी बात अधूरी रह गयी क्योंकि तब तक नीलू उठ कर मेरे सीने पर आ चुकी थी और उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल पास था. उसकी सांसे मेरे चेहरे पर टकरायीं और मैं आगे की बात भूल गया.
``पागल हमने अभी प्यार चखा ही कहां है....क्या पता भरता ही हो....दूसरों की बात मानें या ख़ुद कर के देखें साहब जी....´´ उसकी सांसें मेरे चेहरे पर गर्म नशे की तरह निकल रही थीं और उसकी आंखों में जो था वो मैंने पहली बार देखा था. मेरे मुंह से निकलने वाला था कि ख़ुद करके तब तक उसे होंठ मेरे होंठों से जुड़ चुके थे. पार्क से किसी भी तरह की आवाज़ें आनी बंद हो गयी थीं और मेरे कान में पता नहीं कैसे ट्रेन के इंजन की सीटी सी बजने लगी थी. नीलू ने अपने सीने को मेरे सीने पर दबाया हुआ था और मेरी सांस मेरे भीतर ही कहीं खो गयी थी. जिस ट्रेन की सीटी मेरे कान में बज रही थी मैं उसी की छत पर लेटा हुआ था और हम तेज़ी से कहीं निकलते जा रहे थे. नीलू ने मेरी बांह पकड़ कर अपनी कमर के इर्द-गिर्द लपेट ली. मैंने पहली बार उसकी देह को इतने पास से महसूस किया. मुझे पहली बार ही अहसास हुआ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता. पहली बार ही मुझे अनुभव हुआ कि अगर मेरे सामने वह किसी और की हुयी तो मैं मर जाउंगा. उसने मेरी एक बांह अपनी कमर पर लपेटी थी. मैंने दोनों बांहों से उसे भींच लिया. दूर अठखेलियां करता वह जोड़ा हमें गौर से देख रहा था और कह रहा था कि वो देखो वहां एक जोड़ा अठखेलियां कर रहा है.
थोड़ी देर बाद जब हम नीलू की एक पसंदीदा जगह पर एक नदी के किनारे बैठे थे तो वह मेरी उंगलियां बजाने लगी. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था.
``मगर मुझे नये शहर में नौकरी खोजने में कुछ वक़्त लग सकता है.´´ मेरे मन में अब भी संशय थे और उसके होंठों पर अब भी मुस्कराहट थी.
``एक बात बताओ साहब, तुम्हें बीवी की कमाई खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है.´´ उसकी आवाज़ की शोखी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी सारे संशय उतार फेंकूं और उसके रंग में रंग जाऊं. वह जो मुझे नया जन्म दे रही थी, वह जो मुझे जीना सिखा रही थी, वह जो मेरे सारे आवरणों से अलग कर रही थी.
मैंने उसे झटके से दबोचा और उसी के अंदाज़ में बोला, ``बीवी की कमाई खाने में मुझे बहुत ख़ुशी होगी.´´ मैंने जब उसके होंठों पर होंठ रखे तो नदी का पानी, जो अपने साथ ढेर सारे नये पत्ते बहा कर ले जा रहा था, थम गया और हमें देखने लगा. नदी के होंठों पर मुस्कराहट थी.
हम यह शहर दो दिन के बाद छोड़ देने वाले थे. मुझे पता नहीं था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूं और उदभ्रांत इतनी कम उम्र में इतना समझदार. मैंने हिचकते हुये उसे योजना बतायी तो उसने मुझे बाहों में उठा लिया और कहा, ``तुम जानते नहीं हो भाई कि आज तुमने ज़िंदगी में पहला सही काम किया है. इसके एवज में जो तुम अपने ऊपर उन जाहिलों को बर्दाश्त करने का अपराध करते हो वह भी माफ़ हो जाना चाहिये. उसने मुझे पूरी तरह आश्वस्त किया कि वह यहां सब कुछ संभाल लेगा. उसने बताया कि उसे एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का काम मिल रहा है और कुछ खर्चा वह अपनी उन चार-पांच ट्यूशन्स से निकाल लेगा जिनकी संख्या जल्दी ही और भी बढ़ने का अनुमान है. मैंने बताया कि नीलू वहां जा कर किसी कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी खोजेगी और मैं किसी अख़बार में कोशिश करुंगा. उसने कहा कि उस शहर में उसका एक परिचित दोस्त है जो पेशे से वकील है और सारी औपचारिकताएं पूरी कर देगा. मैंने बहुत लम्बे समय बाद उदभ्रांत से इतनी बातचीत की थी. मैंने उससे कहा कि हम एक दिन अपना घर ज़रूर बनाएंगे. उसने कहा कि उसे ऐसे सपनों में कोई विश्वास नहीं बचा. मैंने कहा कि सपने देखना ही जीना होता है. उसने कहा कि वह किसानों और उनकी ज़मीनों के लिये सपने देख रहा है. पहली बार मुझे उसके सेमिनारों और पोस्टर प्रदर्शनियों की कुछ बातें समझ में आयीं. उसने कहा कि कल वह मेरे ऑफिस आयेगा.
अगली सुबह जब मैं ऑफिस में पहुंचा तो पहुंचते ही `दीन´ जी ने एक गंदा सवाल पूछा, ``मैंने आज तक कभी एक साथ दो महिलाओं के साथ सेक्स नहीं किया. मेरी एक महिला मित्र जिससे मैं सेक्स करता हूं वह दो महिलाओं के साथ प्रयोग करने को तैयार है लेकिन मेरी पत्नी तैयार नहीं हो रही. मैं अपनी पत्नी पर सारे तरीके आज़मा कर देख चुका हूं. मै क्या करूं ?´´ सवाल पूछते हुये वे मेरे काफ़ी करीब तक आ गये थे और अपनेपन से मेरा हाथ पकड़ चुके थे. मैंने उनका हाथ झटकते हुये उन्हें परे धकेला और ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, ``आप अपनी पत्नी को पहले दो मर्दों का आनंद दिलाइये. एक बार उन्हें यह नुस्खा पसंद आ गया तो वह अपने आप मान जाएंगी. फिर आप लोग एक साथ चार, पांच, छह जितने चाहे.....´´ दीन जी मेरी टोन और आवाज़ की ऊंचाई से घबरा से गये और चुपचाप जा कर अपनी सीट पर बैठ गये. वे बेसब्री से बार-बार घड़ी की ओर देख रहे थे. दादा के बिना वे अकेले सिपाही की तरह लग रहे थे. मुझे लगा अभी वह थोड़ी देर में क्रांतिकारी के कमरे में जाकर मेरी चुगली करेंगे लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे और कभी घड़ी तो कभी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखते रहे. मैं जानता था कि उनका सवाल चाहे जैसा भी हो, मैंने उसका जवाब पूरी ईमानदारी के साथ दिया था लेकिन उन्हें जवाब नहीं चाहिये था.
यूपी में है दम क्योंकि जुर्म यहां है कम
दादा के आने के बाद भी `दीन´ जी की भाव-भंगिमा में कोई परिवर्तन नहीं आया हालांकि दादा अपने साथ एक खुशी ले कर आये थे. हमारी पत्रिका को नीले रंग का एक विज्ञापन मिला था और साथ ही यह वादा कि यह विज्ञापन अगले साल के मार्च तक हमारी पत्रिका को मिलता रहेगा. दादा ने थोड़ी देर तक दीन से कुछ बातें कीं फिर सिगरेट पीने बाहर निकल गये. क्रांतिकारी जब तक नहीं आया होता था तब तक ये लोग अंदर-बाहर होते रहते थे. दादा और `दीन´ जी ने उस दिन शाम तक मुझसे कोई बात नहीं की थी हालांकि ऑफि़स में मिठाइयां लाकर बांटने का काम भग्गू ने क्रांतिकारी के फोन के बाद कर दिया था.
शाम के करीब साढ़े सात बजे, जब दादा और `दीन´ को क्रांतिकारी के कमरे में घुसे एक घंटा हो चुका था, मेरा बुलावा आया. भग्गू ने बताया कि साहब ने बुलाया है और दूसरी ख़बर उसने यह दी कि कोई हट्टा-कट्टा लड़का मुझसे मिलने आया है. मैंने उदभ्रांत को खिड़की से भीतर बुलवा लिया. वह मुस्कराता हुआ मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया लेकिन थोड़ी देर बाद ही मुझे अंदर बुलवा लिया गया था. मैं भारी मन से उठा, मैं चाहता था कि आज क्रांतिकारी मुझे न बुलाये और मेरे हाथों बेइज़्ज़त होने से बच जाये.
``तुमने दीन की बेइज़्ज़ती की ?´´ क्रांतिकारी और उसके दोनों चमचों पर तीसरे पैग की लाली तैर रही थी.
``नहीं. मैंने इनके सवाल का जवाब दिया है बस्स, आप पूछ लीजिये इनसे.´´ मैंने सामान्य रहने की कोशिश की.
``साले मेरे सवाल का जवाब दिया कि मेरा हाथ उमेठ दिया, अब तक दर्द कर रहा है.´´ `दीन´ जी चेहरे पर दर्द की पीड़ा ला कर बोले जिसमें से अपमान की परछाईं दिख रही थी. इतने में क्रांतिकारी उठ कर मेरे पास आ चुका था.
``चल तू इतने सवालों के जवाब देता है तो इसका जवाब भी बता. आज तुझे पता चले कि तू अपनी बाप की सगी औलाद नहीं है और तेरा असली बाप मैं हूं जो तेरी मां से मुंह काला करके चला गया था. मैं अचानक तेरे सामने आकर खड़ा हो गया हूं और अब तुझे अपने साथ ले चलना चाहता हूं तो तू क्या करेगा ?´´ क्रन्तिकारी ने अपने हिसाब से काफ़ी रचनात्मक सवाल पूछा था और अब वह एक इससे भी ज़्यादा रचनात्मक उत्तर चाहता था. आज उसके तेवर एकदम बदले हुये थे और आमतौर पर हर बात का मज़ा लेने का उसका लहज़ा बदला लेने पर उतारू मालिक सा लग रहा था. भग्गू आकर दरवाज़े पर खड़ा हो चुका था और इसी पल उदभ्रांत भीतर घुसा.
``बोल क्या करेगा साले बता मेरे.....´´ क्रांतिकारी की बाकी बात उसके मुंह में ही रह गयी क्योंकि उदभ्रांत की लात उसकी जांघों के बीच लगी थी. ``मैं आपके साथ नहीं जाउंगा सर, ऐन वक़्त पर जब आप मेरे काम नहीं आये तो अब क्यों आये हैं. बल्कि मैं तो आपको इस ग़लती की सज़ा दूंगा....´´ मैंने भी उसके पिछवाड़े पर एक लात मारी और वह मेज़ के पास गिर गया. दादा और `दीन´ के चेहरों से तीन पैग की लाली उतर चुकी थी और वे बाहर जाने का रास्ता खोज रहे थे. उदभ्रांत तब तक क्रांतिकारी को तीन-चार करारे जमा चुका था. उसने उसे मारने के लिये तीसरी बार लात उठाया ही था कि वह हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ाने लगा. मैंने उदभ्रांत को रोक कर क्रांतिकारी की जांघों के बीच में एक लात और मारी, ``सर एक और लात मार देता हूं क्या पता आपकी जांघों के बीच में जो शिकायत है वह दूर हो जाये हमेशा के लिये....´´ उसकी डकारने की आवाज़ हलाल होते सूअर जैसी थी.
रात को मैं घर देर से पहुंचा. रास्ते भर मैं और उदभ्रांत हंसते रहे थे और उदभ्रांत ने पहली बार कहा कि अगर कुछ सालों बाद सब ठीक हो गया तो वह एक छोटा सा घर ज़रूर बनायेगा. सब कुछ ठीक होने का मतलब मैं पूरी तरह नहीं समझा था और इसके बाद हम ख़ामोशी से घर पहुंचे थे.
मौसम बहुत अच्छा था और नीलू के साथ ठंडी हवा में उसका हाथ पकड़ कर कुछ दूर चुपचाप
चलने का मन कर रहा था. मैं ख़ुद को भीतर से हीरो जैसा और अद्भुत आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव कर रहा था. नीलू का इतनी रात बाहर निकलना संभव नहीं था इसलिये मैं अकेला ही घूमने लगा यह सोचता हुआ कि आज के सिर्फ़ दो दिन बाद मुझे नीलू का हाथ पकड़ कर घूमने के लिये किसी से कोई इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी. यह सोचना अपने आप में इतना सुखद था कि घर पहुंचने के बाद भी मैं इसके बारे में ही पता नहीं कब तक सोचता रहा. बहुत देर से सोने के कारण सुबह आंख काफ़ी देर से खुली. वह भी मां के चिल्लाने और पिताजी के रोने से. मैं झपट कर बिस्तर से उतरा तो सब कुछ लुट चुका था. तीन जीपों में भर कर पुलिस आयी थी और उदभ्रांत को पकड़ कर ले गयी थी. मैं कुछ न समझ पाने की स्थिति में हक्का-बक्का खड़ा था. मैंने हड़बड़ी में उद्भ्रांत के वकील दोस्त को फोन लगाया तो उसने मुझसे कहा कि मैं जल्दी जा कर केस फाइल होने से रोकूं क्योंकि अगर एक बार केस फाइल हो गया तो उसे बचाने में दिक्कतें हो सकती हैं. मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा कौन सा जुर्म उसने कर दिया कि उसे पकड़ने के लिये पुलिस को तीन जीपें लानी पड़ीं. मैं बदहवासी में पुलिस थाने की ओर भागा. वहां जाकर मुझे पता चला कि उसे पुलिस ने नहीं बल्कि एसटीएफ ने पकड़ा है और उससे मिलने के लिये मुझे किसी फलां की इजाज़त लेनी पड़ेगी. मुझे ही पता है कि उस दस मिनट में मैंने किसके और किस तरह पांव जोड़े कि मुझे वहां ले जाया गया जहां उद्भ्रांत को फिलहाल रखा गया था.
``ये इसका भाई है.´´ मुझे ले जाने वाले हवलदार ने बताया. जींस-टीशर्ट पहने एक आदमी कुर्सी पर रोब से पैर फैलाये बैठा था.
``अच्छा तू ही है अनहद.´´ उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मुझे किसी अनिष्ट की आशंका होने लगी.
``जी....´´ मैं सूखते हलक से इतना ही कह पाया.
``इसे भी अंदर डालो, किताब पर इसका भी नाम लिखा है. थोड़ी देर में कोर्ट ले जाना है, तब तक चाय समोसा बोल दो.´´ उसका इतना कहना था कि मुझे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया.
मुझे एक किताब दिखायी गयी जिसमें नयी कविता के कुछ कवियों की कविताएं संकलित थीं. मैं कुछ समझ पाता उसके पहले उसमें से धूमिल की कविता `नक्सलबाड़ी´ वाला पृष्ठ खोल दिया गया और किताब मेरे सामने कर दी गयी.
``ये तुम्हारी किताब है न ?´´ सवाल आया.
``हां मगर ये तो कविता है. हिंदी के कोर्स में.....´´ मेरा कमज़ोर सा जवाब गया.
``जितना पूछा जाये उतना बोलो. तुम्हारे और तुम्हारे भाई में से हिंदी किसका सबजेक्ट रहा है या है ?´´ सवाल.
``किसी का नहीं. मगर मुझे कविताएं.....´´ मेरी बात काट दी गयी. ``तुम्हारा भाई सरकार विरोधी गतिविधियों में लिप्त है. हमारे पास पुख्ता सबूत हैं. बाकी सबूत जुटाए जा रहे हैं. तुम ऐसी कविताएं पढ़ते हो इसलिये तुम्हें आगाह कर रहा हूं....संभल जाओ. तुम्हारी बाप की उमर का हूं इसलिये प्यार से समझा रहा हूं वरना और कोई होता तो अब तक तुम्हारी गांड़ में डंडा.....´´
मैं समझ नहीं पाया कि मुझे क्यों छोड़ दिया गया. मैं वाकई उद्भ्रांत के कामों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानता कि वह क्या करता था और वह और उसके साथी रात-रात भर क्या पोस्टर बनाते थे और किन चीज़ों का विरोध करते थे, लेकिन मैं यह ज़रूर जानता था कि मेरा भाई एक ऐसी कैद में था जहां से निकलने के सारे रास्ते बंद थे. अगले दिन अख़बारों ने उसकी बड़ी तस्वीरें लगा कर हेडिंग लगायीं थीं `नक्सली गिरफ्तार`, `युवा माओवादी को एसटीएफ ने पकड़ा`, `नक्सल साहित्य के साथ नक्सली धर दबोचा गया´ आदि आदि.
प्रश्न- मैं एक 28 वर्षीय अच्छे घर का युवक हूं. मेरी नौकरी पक्की है और मेरा परिवार भी मुझे बहुत मानता है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अक्सर दुनिया से विरक्ति सी होने लगती है. मुझे सब कुछ छोड़ देने का मन करता है, सारे रिश्ते-नाते खोखले लगने लगते हैं और लगता है जैसे सबसे बड़ा सच है कि मैं दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान हूं. मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि यह स्थिति बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूं ?
उत्तर- छोड़ दो. मत छोड़ो.
इस कदर कायर हूं कि उत्तर प्रदेश हूं
मैंने उद्भ्रांत के वकील दोस्त की मदद से एक अच्छा वकील पाया जिसने पहली सुनवाई पर ही कुछ अच्छी दलीलें पेश कीं लेकिन पुलिस ने अपने दमदार सबूतों से उसे पंद्रह दिन के पुलिस रिमांड पर ले ही लिया. अगली सुनवाई की तारीख पर रिमांड की अवधि बढ़ा दी गयी. अब यह हर बार होता है. उद्भ्रांत ने मुझसे पहली बार मिलने पर ही कहा था, ``भाई मुझे जो अच्छा लगता था, मैंने वही किया. जीने का यही तरीका मुझे ठीक लगा लेकिन घर पर बता देना कि मैं कोई गलत काम नहीं करता था.´´ मैंने सहमते हुये पुलिस की मौजूदगी में उससे धीरे से पूछा था, ``क्या तुम वाकई नक्सली हो ?´´ ``नहीं, मैं नक्सली नहीं बन पाया हूं अभी.´´ वह मुस्कराने लगा और उसने कहा कि मैं घर और मां पिताजी का ध्यान दूं. मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि उद्भ्रांत को किसने गिरफ्तार करवाया होगा. इसका ज़िम्मेदार मैं खुद को मानता हूं. शायद दिनेश क्रांतिकारी ने उस रात की घटना के बाद मेरे भाई को फंसवा दिया होगा. फिर लगता है कहीं नीलू के पापा ने तो अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उसे नहीं पकड़वा दिया ताकि मुझसे बदला ले सकें.
हां, नीलू की शादी की बात तो अधूरी ही छूट गयी. जिस दिन उसकी सगाई होने वाली थी, उस दिन अचानक ऐसी घटना हो गयी कि पूरा मुहल्ला सन्न रह गया. उसके घर में काम करने वाली महरी ने बताया कि रोशनदान से सिर्फ़ पंखे में बंधी रस्सी दिख रही थी और पूरे घर में मातम और हंगामा होने लगा कि नीलू ने आत्महत्या कर ली है. जब पुलिस आयी और उसने दरवाज़ा तोड़ा तो पता चला कि पंखे से एक रस्सी लटक रही है जिसमें एक बड़ी बोरी बंधी है. पुलिस ने बोरी खोली तो उसमें से ढेर सारी नीली शलवार कमीज़ें और एक भारी नीली साड़ी निकली जिसे पहन कर नीलू बी.एड. की क्लास करने जाती थी. मैंने महरी से टोह लेने की बहुत कोशिशें कीं कि वह नीलू के बारे में कुछ और बताये लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था. मैं उस दिन कई बार सोच कर भी उसके घर नहीं जा पाया क्योंकि उस दिन उद्भ्रांत के केस की तारीख थी. पिताजी कहते हैं कि मैं उन्हें भी सुनवाई में ले चलूं. वह अब लकड़ी के सहारे चलने लगे हैं और मैंने उन्हें अगली सुनवाई पर अदालत ले जाने का वादा किया है. वह अजीब-अजीब बातें करते हैं. कभी वह अचानक किसी पुरानी टैक्स फ्री फिल्म का गाना गाने लगते हैं तो कभी अचानक अखबार उठा कर कुछ पढ़ते हुये उसके चीथड़े करने लगते हैं. वह या तो एकदम चुप रहते हैं या फिर बहुत बड़बड़-बड़बड़ बोलते रहते हैं. वह केस की हर तारीख़ पर अदालत जाने की ज़िद करते हैं और मैं हर बार उन्हें अगली बार पर टालता रहता हूं. मां हर तारीख के दिन भगवान को प्रसाद चढ़ाती है और हम लोग जब तक अदालत से लौट नहीं आते, अन्न का एक दाना मुंह में नहीं डालती.
मेरी ज़िंदगी का मकसद सा हो गया है उद्भ्रांत को आज़ाद कराना लेकिन देखता हूं कि मैं तारीख़ पर जाने के सिवा और कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं. उद्भ्रांत का केस देख रहा उसका दोस्त मुझे हर बार आशा देता है और मैं धीरे-धीरे जीतने तो क्या जीने की भी उम्मीद खोता जा रहा हूं. मेरे एक दोस्त ने, जो कल ही दिल्ली से लौटा है, बताया कि उसने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर बिल्कुल नीलू जैसी एक लड़की को देखा है. मैं उससे पूछता हूं कि उसने किस रंग के कपड़े पहने थे तो वह ठीक से याद नहीं कर पा रहा है. बाबा की मौत की ख़बर आयी है और मैंने यह कहलवा दिया है कि अगर उस दिन केस की तारीख नहीं रही तो मैं उनकी तेरहवीं में जाने की कोशिश करुंगा.
मुझे अब नीले रंग से बहुत डर लगता है. मेरे घर से नीले रंग की सारी चीज़ें हटा दी गयीं हैं. मैं बाहर निकलते समय हमेशा काला चश्मा डाल कर निकलता हूं और कभी आसमान की ओर नहीं देखता.
![]() |
| (विमल चन्द्र पाण्डेय) |
प्रश्न-मुझे आजकल एक सपना बहुत परेशान कर रहा है. इस सपने से जागने के बाद मेरे पूरे शरीर से पसीना निकलता है और मेरी धड़कन बहुत तेज़ चल रही होती है. मैं देखता हूं कि मेरा एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा बगीचा है जिसमें दरख़्तों की डालें सोने की हैं. उन दरख्तों में से एक पर मुझे उल्लू बैठा दिखायी देता है और मैं अपना बगीचा बरबाद होने के डर से उल्लू पर पत्थर मारने और रोने लगता हूं. तभी मुझे सभी डालियों से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं और मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूं, पाता हूं कि हर डाली पर उल्लू बैठे हुये हैं. इसके बाद भयानक ख़ौफ़ से मेरी नींद खुल जाती है. मैं क्या करूं ?