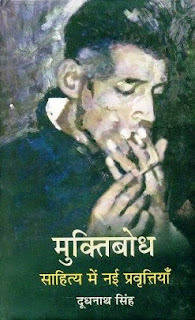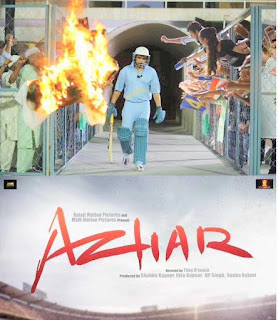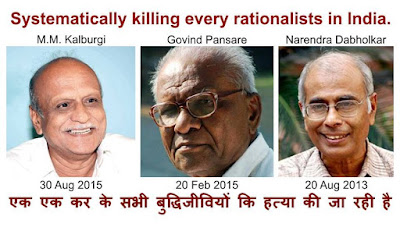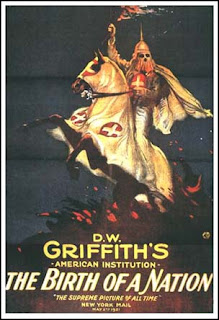समकालीन हिंदी आलोचना में प्रभात की कविताओं को लेकर उत्साह है, हालाँकि अभी उनका एक ही काव्य-संग्रह ‘अपनों में नहीं रह पाने का गीत’ प्रकाशित है. कविताओं के अतरिक्त आदिवासी लोक साहित्य पर भी उनका कार्य है और बच्चों की रचनात्मक दुनिया में भी उनकी उपस्थिति है. प्रमोद कुमार तिवारी ने कवि प्रभात की ‘निजता’ और ‘विशिष्टता’ को विस्तार से देखा-परखा है.
दु:ख! क्या सच में मुक्ति देता है?
प्रमोद कुमार तिवारी
![]()
एक ऐसे दौर में जब साहित्य के नाम पर सबसे ज्यादा कविताएं मौजूद हों,जब पुराने-नये सभी जन माध्यमों में कविताओं की लगभग बाढ़ सी आयी हो और ज्यादातर लोगों के पास समय का अभाव हो तो सामान्य सा सवाल उठता है कि कोई कविता क्यों पढ़े? और शीघ्र ही यह सवाल इस रूप में सामने आ जाता है कि कविता की जरूरत ही क्या है? कथा,उपन्यास,सिनेमा आदि से साहित्य का काम पूरा हो रहा है अलग से कविता को क्यों महत्व दिया जाय?
कविताओं से लगभग ऊब के इस समय में प्रभात की कविताएं अचानक फूटे शोक के किसी सोते की तरह लगती हैं. ऐसा लगता ही नहीं कि ये कविताएं छपाने,सुनाने या किसी को बताने के लिए लिखी गई हैं बल्कि ये लगभग आत्मालाप की तरह हैं जिसमें कवि अपने दुख को खुद से ही कह - कह कर अपना मन हल्का कर रहा है. ये कविताएं अनायास ही पाठक को जीवन के उस धरातल पर पहुंचा देती हैं जहां आत्म और पर के बीच का,होने और न होने के बीच का फर्क मिटता सा नजर आता है. लेकिन इन बातों से यह अर्थ बिलकुल न निकाला जाय कि ये कविताएं आध्यात्मिक या पराभौतिक हैं. इनमें बिलकुल सामने का ठेठ जीवन है. घनघोर सांसारिकता से भरा पूरा. इसके बावजूद ये कविताएं वर्तमान समय की विमर्श केंद्रित कविताओं से बिलकुल अलग खड़ी हैं.
जब साहित्य अकादेमीसे प्रकाशित प्रभातका कविता संग्रह हाथ में आया तो इसका नाम ‘अपनों में नहीं रह पाने का गीत’कुछ अटपटा सा लगा. खास तौर से तब जब कि इस संग्रह में ‘अपनों केनहीं रह पाने’के ढेर सारे गीत मौजूद हैं,परंतु यहीं से प्रभात का ‘प्रभातपन’खुलना शुरू होता है. प्रभात का अनुभव संसार,निरीक्षण शैली,यूं कहें कि प्रभात की नजर कुछ भिन्न प्रकार की है,बातों को ये प्रचलित ढंग से नहीं उठाते. न सुख को ‘सुख’की तरह देखते हैं और न दुख को ‘दुख’की तरह. इस संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुख के भीतर दुख पैठा है और दुख भी खालिश दुख नहीं,उसमें सुख की छुवन है.
‘शबे हिज्र थी यूं तो मगर पिछली रात को
वो दर्द उठा फिराक़ कि मैं मुस्कुरा दिया’
काव्यशास्त्रीय व्याख्याओं के अनुसार जब सामाजिक के चित्त में विकास और विस्तार होता है तो उसे सुख मिलता है और क्षोभ और विक्षेप होता है तो दुख. परंतु क्या दुख विस्तार नहीं करता है? साहित्य से उत्पन्न होनेवाले क्षोभ क्या लौकिक या सांसारिक क्षोभ जैसे ही होते हैं? या फिर,क्या दुख आनंददायक भी हो सकता है? बहुत पहले रस के स्वरूप की व्याख्या करते समय रामचंद्र गुणचंद्रने ‘सुख दुखात्मो रस:’कहा था. यानी जीवन की तरह कविता भी इन दोनों के बीच खड़ी है बल्कि दुख की ओर थोड़ा ज्यादा झुकी हुई. बुद्ध ने भी जीवन को दुखों का सागर कहा था और दुनिया के ज्यादातर (और भारत के भी रामायण और महाभारत दोनों) महाकाव्य दुखांत हैं. एको रस: करूण: कहकर भवभूति ने भी दुख की निरंतरता को स्थापित किया है. प्रभात के संग्रह से गुजरते समय ये सारे संदर्भ अनायास ही दिमाग में चले आते हैं क्योंकि यह संग्रह दुख की ओर झुका हुआ है और लगभग एक शोकगीत की तरह है. परंतु यह दुख वेदना या पीड़ा नहीं है,ठीक वैसे ही जैसे कि सुख आनंद नहीं है.
प्रभात एक संक्रांति का निर्माण करते हैं- सुख और दुख की संक्रांति,रोने और हंसने की संक्रांति,संलिप्तता और निर्लिप्तता की संक्रांति,संबंधों में प्रगाढ़ता और मुक्ति की संक्रांति या यूं कहें कि वे ‘जीवन जैसा जीवन’कविता में रचने की कोशिश करते हैं. इस प्रयास में कई बार सार्थकता और निरर्थकता की सीमाओं को तोड़ कर एक तरह का एब्स्ट्रेक्ट रचते हैं,लगभग पेंटिंग की तरह. बस कुछ है,एक स्पेस है,उसमें अर्थ की खोज करना एक खास तरह की निर्ममता जैसी लगती है. जैसे किसी बच्चे के नॉनसेंस को तर्क की कसौटी पर कसना नॉनसेंस से कई गुना बड़ा नॉनसेंस,लगभग सेंसलेस,लगता है. क्या कविता से पेंटिंग या खयाल गायकी के उस स्तर तक पहुंचा जा सकता है जहां शब्द नहीं बस रंगों या स्वरों की अनुगूंज शेष रह जाए. कुछ महसूस हो,ऐसा जो आपकी मानसिक भावभूमि को एक ऊंचाई प्रदान करे,जहां अच्छा है या बुरा है यह बेमानी हो जाए बस होना शेष रहे. लेकिन स्वरों के इस उठान के लिए बड़ी साधना की दरकार होती है.
कब सपाटबयानी का विवादी स्वर पूरी लय को बिगाड़ देगा,कब आत्मकेंद्रिकता का वर्जित स्वर सुर के पूरे महल को धराशायी कर देगा कहना मुश्किल है. प्रभात की विशिष्टता इसी बात में है कि ढेर सारी सुर लहरियों के बावजूद कहीं बेसुरापन नहीं आने देते. इन्हें पढ़ते हुए लगता है मानो आप एक विशालकाय लहर पर सवार हों जो कभी भीतर डुबोती है,कभी सतह पर फेंकती है,कभी हिचकोले लगाती है तो कभी तली में बैठा देती है,ऐसी तली जहां अपनी ही धड़कन कानों में बजने लगे. ऐसी तली जहां शोक,श्लोक और आनंद एक ही धरातल पर उतर आएं. जहां सत्ता के दुष्चक्र हास्यास्पद से लगने लगें. जहां हजारों बार की देखी-सुनी,जानी-पहचानी झाड़ू अचानक मनुष्यता और सभ्यता के प्रतीक चिह्न में तब्दील हो जाए.
जहां झाड़ू के बुहारने,सफाई करने,स्वच्छ बनाने आदि का ऐसा अपूर्व उदात्तीकरण हो जाए कि निराला के कुकुरमुत्ता की तरह झाड़ू ‘झाड़ू’मात्र न रहकर कुछ और बन जाए. सामान्य सी झाड़ू इतनी अभौतिक,इतनी अशरीरी हो जाए कि उसे आत्मा से लेकर सपनों तक पर फेरा जा सके,जिस पर सवार होकर दुनिया के किसी भी विषय की यात्रा की जा सके. जिसका होना मनुष्यता के होने,जिंदा होने यहां तक कि ‘न होने के होने’की भी पहचान बन जाए. ‘न होने का होना’क्या है इसे छोटी सी कविता ‘श्मशान’में देखा जा सकता है-
यह निवास है उन प्राणियों का
जिनकी सांस की लय टूट गई
जिनके स्वरूप का कोई स्वरूप नहीं रह गया
जो होने से विहीन हो गए.......
अस्थियों की राख की बस्ती
डेरा है नश्वरों का
इसमें जाया जाएगा
लेकिन जाया नहीं जा सकता
प्रभात की कविताएं पिछले 10-15 वर्षों के दौरान लिखी गई कविताएं हैं सो उनमें वर्तमान समय की स्पष्ट आहट महसूस की जा सकती है,स्त्री,पर्यावरण,उपेक्षित आदि के विमर्श और प्रतिरोध को भी देखा जा सकता है. परंतु प्रतिरोध इतना शांत,इतना थिराया हुआ और इतना निर्लिप्त भी हो सकता है ये प्रभात बताते हैं. विमर्शों के राजनीतिक शोर से बहुत दूर एक प्रकार का हाहाकार इन पंक्तियों में बंद है. उदाहरण के लिए 85 कविताओं के इस संग्रह में स्त्री से संबंधित,स्त्री को संबोधित अनेक कविताएं हैं- मृत फूफा के साथ पूरे गांव में अकेली बुआ,फांसी लगा फंदे से झूल गयी बहन,तीन बच्चों को श्मशान पहुंचाने के बाद खुद वहां पहुंचनेवाली मां,कभी नहीं मरनेवाली बुढिया सईदन चाची,सती बनाई जाती शकुंतला आदि आदि. और इनके अलावे लोकगीत गाती स्त्रियां,ऊंटगाड़ी में बैठी स्त्रियां,समारोह में मिलीं स्त्रियां,पानी ढोती स्त्रियां. यानी स्त्रियों के अनेक चित्र है पर अपारंपरिक से,कुछ अनूठापन लिए हुए. यहां स्त्री की पीड़ा है,तंत्र द्वारा निर्मित कुचक्र हैं,स्पष्ट पक्षधरता है,स्त्री के साथ हो रहे अन्याय पर चित्कार कर रहा संवेदनशील पुरुष भी है परंतु विमर्श का एकांगी या कहें लगभग पुरुषविरोधी शोर नहीं है. लगभग मरणासन्न स्त्री और पुरुष एक दूसरे से लिपट कर जीवन के चरम संघर्ष को अपने प्रेम से जीतते हैं-
कैसे टला आत्महत्या का संगीन प्रसंग
कैसे एक भूखा आदमी/ एक भूखी औरत से लिपटा
अन्न जल जैसी असंभाव्य वस्तुएं पाता रहा
उसकी आश्रय-भरी बातों से.
हालांकि कवि जानता है कि घनघोर श्रम के बावजूद स्त्रियों के लिए सुख का ठौर नहीं है. सुख के शहर तक पहुंचने के लिए वह रेल में बैठती है,नये नये स्थान का सफर करती है और हर बार पहले से घना दुख पाती है. ऐसा क्यों है कि संग्रह में जब स्त्रियां आती हैं तो अक्सर उनके साथ मृत्यु और रूदन के प्रसंग खींचे चले आते हैं? क्या इसे पलट कर देखने की जरूरत है,कि मनुष्य के संदर्भ में स्त्री के प्रसंग सबसे ज्यादा जीवन के प्रसंग हैं और कवि इस जीवन को मरण से जोड़कर स्त्रियों से जुड़ी सामाजिक विडंबना को चित्रित कर रहा है. ‘स्त्री जीवन के दुर्भिक्ष के गिद्धों’को बेनकाब करने का कहीं यह सायास प्रयास तो नहीं है. जबरन सती बनाई जाती ‘शकुंतला’कविता में ऐतिहासिक नाम और सदियों पुरानी परंपरा की दुहाई देता कवि स्पष्ट कहता है -
‘राजपुताने में तुझ अकेली का नहीं फूटा है भाग....
तू यहां नहीं/ किसी खपरैल में जन्मी होती
कालबेलियों में नहीं नगर में जन्मी होती...
समुद्र के इस पार नहीं/ उस पार जन्मी होती
ब्राह्मण से ब्राह्मण/ दलित से दलित / सभी वर्णों में होती
तू भाइयों की मां जायी दासी
घर को खा जाने वाली बैरन ननद.’
किसी कवि की महत्ता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि वह जीवन तत्त्व को कितना पकड़ पाया है. जिस प्रकार मनुष्य के संदर्भ में स्त्री का प्रसंग जीवन से जुड़ता है उसी प्रकार जैविक संदर्भ में यह जीवन सबसे ज्यादा पानी से जुड़ता है. जीवन तत्त्व को जल तत्त्व भी कहा जा सकता है. प्रभात के यहां जल के बिंब बार बार आते हैं,बिलकुल भिन्न संदर्भों में. पानी की तरह कम तुम,जोहड़,पानी की बस्ती,पानी की इच्छाएं,पानी की बेल,तालाब,नदीजैसी पानी को नये आयाम देती हुई ढेर सारी कविताएं हैं और मजे की बात यह कि पानी की शिकायत खुद पानी से ही करता हुआ पानीदार कवि भी है-
‘मैं तुम्हें मेरे लिए पानी की तरह कम होते देख रहा हूं
मेरे गेहूं की जड़ों के लिए तुम्हारा कम पड़ जाना
मेरी चिडि़यों के नहाने के लिए तुम्हारा कम पड़ जाना...
मेरी आटा गूंदती स्त्री के घड़े में तुम्हारा नीचे सरक जाना
तुम्हारे व्यवहार में मैं यह सब होते देख रहा हूं’
और जिन कविताओं में पानी सीधे-सीधे नहीं आ रहा है वहां भी वह आ जाता है मसलन एक दुर्लभ कविता है ‘धरोहर’जिसमें पानी के संकट पर अखबार में लिखे जाने पर खुद्दारी से भरा वृद्ध किसान अफसोस से भर जाता है और कहता है कि ‘कोई पढ़ेगा तो क्या कहेगा/ कैसा अभागा गांव है वह जिसमें पानी नहीं है.’
इस अफसोस का,खराब से खराब परिस्थिति में भी अपने गांव,अपने घर,अपने लोगों की खराब छवि न बर्दाश्त कर पाने की आदत का गहरा रिश्ता उस संपृक्ति बोध से जुड़ता है जिसे लंबे अनुभव के बाद लोक ने अर्जित किया था. संभव है,आज के तेज भागते,उपलब्धियां बटोरते महानगरीय परिवेश में ऐसे पात्रों का रचा जाना ही नहीं कुछ समय बाद समझा जाना भी मुश्किल हो जाए. ‘अपनों में नहीं रह पाने का गीत’जैसी रचनाएं सिर्फ वैज्ञानिक विकास से सफलता मापती दुनिया में संभव नहीं हो सकती हैं. यह अनायास नहीं है कि इस संग्रह में किसानों के अनेक चित्र आते हैं – किसान…गायब होते किसान... हार मानते किसान…मजदूर बनते किसान…ढहते-गिरते पस्त होते,गायब होते किसान... और इन किसानों के पक्ष में खड़ा कवि. ध्यान दें किसानों के इन चित्रों में हुलास नहीं है,लगातार पलायन करते,आत्महत्या करते किसानों की छवि इन पस्त चित्रों में देखी जा सकती है. तमाम चीजों की तरह किसान शब्द भी लगातार सीमित होता गया है,किसान खेतों में काम करनेवाला मात्र एक श्रमिक नहीं है. किसान का मामला केवल अन्न उत्पादन और आर्थिक समृद्धि से जुड़ा मामला नहीं है. किसानी केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वह भारत की लगभग 65.7 फीसदी आबादी का पेट पालती है. किसानी एक संस्कृति है. इस संस्कृति का संबंध प्रकृति,भाषा,त्योहार,जीवन संगीत,आत्मनिर्भरता आदि विविध जीवन-पक्षों से जुड़ता है.
इन सब के बीच एक लय बिठाता है किसान. यह यूं ही नहीं है,कि नकदी फसलों और लाभ के गणित से संचालित तुलनात्मक रूप से सक्षम किसान बिहार के गरीब किसानों की तुलना में ज्यादा हताशा (कई बार आत्महत्या की सीमा तक) महसूस करते हैं क्योकि पूंजी के दबाव में जीवन संगीत से उनकी लय टूट रही होती है. कवि अन्न उत्पादक किसानों तक सीमित नहीं है,उसकी बड़ी चिंता टूटते संबंध,बिखरते गांव और किसानी से जुड़ी मनुष्यता के लगातार क्षरित होने की है. ये कविताएं नास्ट्रेल्जिया से कोसों दूर हैं और गांवों के भीतर की कुरूपता,वहां के घात-प्रतिघात को भी बयां करती हैं -
जिस गांव की सुखद स्मृतियां सपनों में आती हैं
उसी गांव में जाते अब डर लगता है
शहर या दूर के लोगों से कैसी शिकायत,जो अपने थे उनकी भयावह दूरी असहनीय हो जाती है. सवाल शहर-गांव,उद्योग या किसानी का है ही नहीं,सवाल मनुष्य,प्रकृति और जमीन से उस रिश्ते का है जो लगातार छीजता जा रहा है-
अभी-अभी तक जो सहचर थे सुख-दुख के
पढ़-लिखकर दूर के हो गए वे
हुजूर और गुलाम का रिश्ता हो गया उनसे...
भरी पंचायत में ललकार सकते थे जिन्हें
कंधा पकड़कर नीचे बैठा सकते थे अनीति करने पर
प्राण हलक को आ जाते हैं थाने अस्पताल कोर्ट कचहरी में
भूल से कहीं उनसे टकरा जाने पर
इस संग्रह में जो एक दुख की टेक है उसके मूल में प्रकृति सहचर किसानों की दुर्दशा भी है. और इस दुर्दशा की करूण गाथा कहते कवि की स्पष्ट पक्षधरता भी है. निश्चित रूप से प्रभात इस करुणा और विडंबना से गहरे व्यंग्य का सृजन करने में सफल होते हैं. यह व्यंग्य अखबारों और मंचीय कविताओं में दिखनेवाला व्यंग्य नहीं है,बहुत ही खामोश और नीरव व्यंग्य,समाज की चूलों को हिलाता हुआ . एक उदाहरण देखा जा सकता है
‘जब-जब भी मैं हारता हूं
मुझे स्त्रियों की याद आती है
और ताकत मिलती है
वे सदा हारी हुई परिस्थितियों में ही / काम करती हैं...
वे काम के बदले नाम से/ गहराई तक मुक्त दिखलाई पड़ती हैं
असल में वे निचुड़ने की हद तक/ थक जाने के बाद भी
इसी कारण से हँस पाती हैं/ कि वे हारी हुई हैं
विजय-सरीखी तुच्छ लालसाओं पर उन्हें/ ऐतिहासिक विजय हासिल है.’
असल में वह किसान पर हो या स्त्री पर,इस संग्रह की ज्यादातर कविताएं व्यंग्य कविताएं हैं. वह व्यंग्य नहीं जो सपाट सा विपक्ष रचता है,जो किसी को हास्य और किसी को क्षोभ या गुस्सा देता है. यहां ऐसा व्यंग्य है जो इन दोनों से दूर उस त्रासदी तक ले जाता है जहां आप अपने भीतर कुछ चिनकता सा,कुछ टूटता सा महसूस करते हैं. एक शोक की भावभूमि जहां एक ही बात शेष रह जाती है कि ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता. कुछ ऐसा जैसा प्रेमचंद ‘होरी’की मृत्यु से निर्मित करते हैं. ऐसी स्थिति जहां सारी भौतिक उपलब्धियां पाया हुआ अहं से भरा,गांव से निकल बड़ा अधिकारी बन चुका व्यक्ति अपने निरर्थकता बोध से इस सीमा तक संतप्त हो जाता है कि खुद को ‘मृत्यु का छोड़ा हुआ’महसूस करने लगता है –
उसे लगा मैं घर में घरवालों का
बाहर,बाहर वालों का छोड़ा हुआ हूं
अच्छा और बुरा लगने का छोड़ा हुआ हूं
सार्थकताओं और निरर्थकताओं का छोड़ा हुआ हूं
उसे लगा जीवन नहीं हूं मैं एक
मृत्यु का छोड़ा हुआ हूं महज
यहां नकार या आक्रामकता नहीं है,बल्कि इनके होने से व्यंग्य कमजोर होता है. सामनवाले के मारने पर वह चोट कभी नहीं लगती जो आपके भीतरवाले के मारने से लगती है.
एक साधारण सा सवाल मन में आता है कि प्रभात में इतना मृत्यु बोध क्यों है,बार बार कविताओं में मृत्यु क्यों आती है? इसका एक खिलंदड़ा सा उत्तर हो सकता है कि जिन परिस्थितियों में गांवों में किसान,स्त्रियां,बेरोजगार रह रहे हैं उनमें भला और कौन-सा बोध आएगा. परंतु प्रभात इतने सरल कवि नहीं हैं,अपनी तमाम सहजताओं के बावजूद वे किसी भी विषय का सरलीकरण नहीं करते. वह चाहे कैसा भी विषय हो लाउडनेस नहीं आने देते. असल में हर बड़ी कविता मृत्यु से टकराती है. ट्रीटमेंट का अंतर हो सकता है परंतु इस कठोर सच्चाई का सामना तो करना ही पड़ता है खास तौर से तब,जब आप विज्ञान और पूंजी के बनाए ‘सुद्दोधन महल’में सिद्धार्थ की तरह न रहकर ‘बुद्ध’की तरह रहना चाहते हों. तब मृत्यु से टकराए बगैर आपका काम नहीं चल सकता. प्रभात की कविताओं में मृत्यु के अनेक शेड्स हैं,सुख दुख से परे किसी और भूमि पर टिके हुए. ‘मृत्यु के दिन क्या होगा/ कुछ खास न होगा/ और दिनों-सा गुजर जाएगा/ और यह रात गर्भ-सी होगी/ दिन का चूज़ा कुनमुनाएगा.’
मृत्यु भी कैसी?केवल इंसानों की नहीं,परिंदे,कीड़े,कुर्ते,धोती,अंगोछे,पेड़ जाने किस-किस की. और सबके शोक में कवि शामिल है. शामिल होना भी चाहिए वरना कवि क्या हुआ फिर. क्या कविता शोक के भारी वजन को उठाने के लिए अड़ी हुई कंधे की तरह है. जहां कोई दुखी दिखा वहां पहुंच जाती है उसके कंधे पर हाथ रखने. हाथ रखने के अलावे भला वह और कर भी क्या सकती है? परंतु क्या यह हाथ रखना मामूली काम है?
इसमें दो राय नहीं कि प्रभात कवि परंपरा के नैसर्गिक वारिस हैं,इसके कई प्रमाण इस संग्रह में मिलते हैं. एक रचनाकार सबसे पहले और सबसे ज्यादा सौंदर्य प्रेमी होता है या कहें जिस अनुपात में सौंदर्यप्रेमी होता है उसी अनुपात में कुरूपता विरोधी भी होता है.
‘विशाल हवा का झाड़ू चाहिए ही
पृथ्वी पर फैली असुंदरताओं को बुहारने के लिए
प्रभात का सौंदर्यबोध थोड़े भिन्न किस्म का है जो उनके विषयों के चयन में भी नजर आता है. विषयों का यह अलहदापन कहां से आता है,इतने नवीन विषय कहां से लाते हैं प्रभात? असल में यह विषयों का नयापन नहीं दृष्टि का नयापन है,बोध का नयापन है. विषय तो वही हैं,देखने का और प्रस्तुतिकरण का ढंग नया है. प्रभात ने साधारण के भीतर की असाधारणता को उकेरने का ढंग निकाल लिया है. विचारों को बहुत ही सरल ढंग से दैनिक जीवन के नामालूम से प्रसंगों से जोड़ देने का सलीका निकाल लिया है. प्रभात ढेर सारे ऐसे संदर्भ रचते हैं जहां एक बड़ी बात इतनी सादगी से कह दी जाती है कि सहसा यकीन ही नहीं होता कि इसे इतनी सरलता से भी कहा जा सकता है. तीन पंक्तियों की एक कविता है ‘सुख-दुख’
उनकी अपनी किस्म की अराजकता है मेरे भीतर
सिर्फ दुखों की नहीं है
सुखों की भी है
या फिर धाड़ैती पर भी कविता लिखी जा सकती है और इस विषय को इतना तरल बनाया जा सकता है. या विरक्ति को ‘अकेले आदमी की बस्ती’के रूप में भी देखा जा सकता है. किसी बस्ती में अकेला आदमी हो तो वह कैसी बस्ती होगी,उसके भीतर कितनी असहायता और घुटन होगी? विरक्त व्यक्ति किन मजबूरियों में ऐसा होने का निर्णय करता होगा? इन सब के बावजूद उम्मीद है,कवि निराश नहीं है,एक कवि निराश होता भी नहीं है. आधी से अधिक रात के बीत जाने पर भी अपराध जगत के गलियारों और षड्यंत्रों में बेचैन राजनेताओं के बंगलों से बहुत दूर,दुनिया पर हावी होना चाहने वाले जगत से दूर एक कमरे की लाइट का जलना,विचारमग्न युवक का होना एक बड़ी उम्मीद है. सारी साजिशों,सारी कुरुपताओं के बरक्स किसी का खड़ा होना आशा का संचार करता है. इसी संग्रह में ‘कोई भी चीज लंबी नहीं चलती’जैसी कविता भी है.
‘कोई भी चीज इतनी लंबी नहीं चलती
न खामोशी लंबी चलती है/ न आंसुओं की झड़ी
न अट्टहास/ न हँसी/ न उम्मीद न बेबसी...
और-और तरीकों से
पूँजी के बिना भी जीते हैं लोग
गाते हुए गीत और लोरियाँ .’
प्रतिरोध का ऐसा सरल रूप... दिमाग में फैज का ‘हम देखेंगे’और ब्रेख्त का ‘जनरल तुम्हारा टैंक बहुत मजबूत है’जैसी कविताएं अनायास चली आती हैं. सारी साजिशों के विपक्ष में लोरियों का खड़ा होना कितने लंबी और बड़ी उम्मीद की ओर संकेत करता है,इसे सहज ही समझा जा सकता है. बिना किसी तेवर के अत्यंत महीन संकेत में, नंगे पांव कच्ची पगडंडियों से पक्की सड़क की ओर जाते बच्चों के बहाने,कवि कहता है-
इनके फूल से तलुवों को
ठंड की आंच में सिंकते देखते हुए
मैं इतना ही कह रहा था
गांव में फूल नहीं खिलते
आग खिलती है
प्रभात सहज कवि हैं परंतु बहुत सचेत कवि भी हैं. बिना ऐसी सचेतनता के झाड़ू जैसी कविता संभव ही नहीं हो सकती. 16 पृष्ठों में विभाजित ‘झाड़ू’को हिन्दी कविता की उपलब्धि कहने का मन होता है. सूचना क्रांति द्वारा निर्मित कृत्रिम विराटता के भीतर से झांकती एक खास तरह की लघुता के इस दौर में,जहां हर चीज का सामान्यीकरण किया जा रहा हो,जब केवल दूरी और समय को ही नहीं हर चीज को रिड्यूस करने को,उसे एकरूप-एकांगी बना देने को एक उपलब्धि मान लिया जा रहा हो,जिसमें संबंध,प्रकृति,राजनीति,विमर्श सब कुछ धीरे-धीरे शामिल होता जा रहा हो,ऐसे समय में एक नामालूम सी वस्तु ‘झाड़ू’को विराट बना देना उल्लेखनीय लगता है. किसी भी चीज को प्रतीक बनाया जा सकता है,महत्वपूर्ण यह है कि वह प्रतीक हमारी चेतना को कितना विस्तार देता है. झाड़ू नाम लेते ही तमाम राजनेता,दल,सफाई आदि की छवि मानस में तैर जाती है,लेकिन यह छवि एकांगी है लगभग एक रूढि़ की तरह,प्रभात अपने झाड़ू से इस रूढि को तोड़ देते हैं. उसे विस्तार देते हैं,उसे सभ्यता और श्रम का अभिन्न अंग बना देते हैं. 21 खंडों में विभाजित यह कविता एक ही अंत:सूत्र में गुंथी हुई है. इतनी गझिन,इतनी गठी हुई कि इसके बीच से होकर निकलने में पाठक को अच्छा खासा समय लग सकता है. जाने कितने प्रकार की झाड़ू,सिंक की,खजूर की,दूब की,शब्द की,लोहे की,बारिश की,जीभ की,हवा की,रोशनी की झाड़ू. एक महाकाव्यात्मक औदात्य की कविता रचने में सफल हुए हैं प्रभात.
‘दुनिया के सभी झाड़ू
दुनिया के हाथों के छोटे भाई हैं
जब झाड़ू नहीं थे
हाथ झाड़ू का काम करते थे
इकलौते नहीं कहे जा सकते अब हाथ
इंसान के हाथ में झाड़ू आ जाने के बाद.’
झाड़ू को प्रभात ने भी प्रतीक बनाया है पर एक की जगह अनेक का प्रतीक बनाकर उसे किसी खास घेरे में बंधने से बचा लिया है. पर निराकार भी नहीं होने दिया है,आकार और पक्ष स्पष्ट है-
‘झाड़ू की तरह पड़े रहते हैं लोग
दुनिया के ओनों-कोनों में
लेकिन सुबह होते ही
दुनिया को उनकी जरूरत पड़ती है...
जैसे ही पुल बन जाते हैं
जैसे ही बांध बन जाते हैं
उन्हीं ओनों-कोनों में फेंक दिया जाता है लोगों को
जहां से खदेड़कर लाया गया था...
एक दिन ऊब जाते हैं लोग इन क्रूरताओं से
इंकार कर देते हैं इनमें रहने-सहने से
इन लोगों की सांसे इकट्ठी होकर
धरती पर एक विशाल हवा को खड़ा करती हैं’
और फिर उस विशाल हवा के झाड़ू से बुहार दिए जाते हैं बड़े से बड़े मठ,बड़ी से बड़ी सत्ताएं,यह कहने से कवि खुद को बचा लेता है.यह सचेतनता महत्वपूर्ण है. एक बिंदु पर कितनी देर टिका जा सकता है,इसके लिए कितनी एकाग्रता जरूरी होती है,झाड़ू कितने दिनों तक कवि मन में चली होगी,यह टिकाव बहुत महत्वपूर्ण है.
प्रभात के यहां शब्द और भाषा का खिलवाड़ जबरदस्त है परंतु सिर्फ खेल के लिए नहीं,इस खिलंदड़ेपन में सार्थकता का छोर कभी छूटने नहीं पाता. वाक्यों का क्रम भंग,अपरंपरागत ढंग से उनका टूटना,परसर्गों का बेहतरीन इस्तेमाल. विरोधाभास (उनके लहंगों का वजन/ उनकी सूखी जंघाओं से कहीं अधिक था/ उनकी पीली ओढ़नियां भड़कीली थीं/ मगर उनसे ढंके उनके झुर्री पड़े चेहरे/ बुझी राख थे) के माध्यम से ढेर सारी बातें कम शब्दों में समेट लेने की अदा. ऐसी अनेक कविताएं हैं जिन्हें पढ़ के कवि के उर्दू शायरी की परंपरा से जुड़े होने का पता चलता है. मृत्यु के बाद ‘जाने कहां’चले जाने पर एक छोटी सी टिप्पणी-
‘जाना भी कहां वह गया जहां
वह कुछ भी कहां कि जाया जा सके वहां’
बिलकुल नये बिंब,नयी वाक्य संरचनाओं से लबरेज इन कविताओं की सबसे खास बात यह है कि इनमें टुकड़ों में चमकती पंक्तियां नहीं हैं,कविता अपने पूरे वितान में मौजूद है.
यह संग्रह इसलिए महत्वपूर्ण है कि कवि जी-जान से लगा हुआ है सुंदरता की तलाश में,अथाह प्रेम भरा हुआ है इसमें. ढेर सारी कविताओं में यह प्रेम बाहर छलक पड़ता है और जिनमें सतह पर नहीं दिखता उनमें भी थोड़ा कुरेदने पर उसे महसूसा जा सकता है. इतने विकट समय में वह प्रेम ही है जो उर्जा दे रहा है. जो पेड़ तक को प्रेमिका बनाए दे रहा है.
प्रभात का प्रभातपन इस बात में निहित है कि यह कवि अपनी उम्र और ज्ञान को खुद से परे
रख पाने में सफलता हासिल कर लेता है. करुणा की जिस भाव भूमि पर ये कविताएं स्थित हैं वह बिना ‘मैं’को छोड़े तैयार ही नहीं हो सकती. चमकदार,चर्चित साहित्यिक दुनिया में प्रभात के अल्पज्ञात होने में भी इस ‘मैं’के विलोप की भूमिका हो सकती है. यह कवि ‘सार्थकता की बौद्धिक मांगों की निरर्थकता’को समझता हैऔर एक बड़े समूह द्वारा निरर्थक मान लिए गए प्रसंगों की मनुष्य और मनुष्यतर संबंधों में सार्थकता को न केवल समझता है बल्कि उसे बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता भी रखता है.
प्रभात में लगभग शिशु की तरह चीजों को पहली-पहली बार अपनी तरह से देखने की क्षमता है. इसीलिए वे प्रचलित मुहावरों और रूढ़ भाषा से मुक्त रह पाते हैं. इस संग्रह की सार्थकता इस बात में है कि यहां कवि नहीं है,कवि की जगह एक कैमरा है जिसे बहुत ही उपयुक्त जगहों पर फिट कर दिया गया है. वह कैमरा कभी पूरे गांव में अकेली बची स्त्री को दिखा रहा होता है,कभी दिमाग में चल रहे उथल-पुथल को पकड़ रहा होता है, कभी मुआवजा के बदले आंसू गैस देते,बुलडोजर चलाते तंत्र को पकड़ रहा होता है तो कभी अंतिम सांसे गिन रहे बबूल के पेड़ पर फोकस हो जाता है. कैमरा जैसा निर्लिप्त होता है,जैसा होना चाहिए वह इन कविताओं में है. पर कैमरे को कहां रखना है,उससे क्या और किसे दिखाना है,इसे लेकर कोई दुविधा नहीं है. कवि की वैचारिकता,उसकी पक्षधरता एकदम स्पष्ट है. शायद इन कविताओं के अलहदेपन के मूल में यही ‘सपक्ष निर्लिप्तता’है. कवि की निगाह कहां है इसका पता एक छोटी सी कविता देती है जिसमें गांव से दो घर (एक घर प्रेम के कारण और दूसरा गरीबी के कारण) उजड़ जाते हैं परंतु कवि उनके उजड़ने की बात से उदास नहीं होता जितनी इस बात से कि
‘क्यों उजड़ गए गांव से दो घर
किसी ने नहीं पूछा किसी से’
समाज से पूछा गया पृथ्वी सा भारी यह ‘क्यों’महत्वपूर्ण है और प्रभातपन की पहचान भी. इस संग्रह की सीमाएं मुझे नजर नहीं आयीं इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि सीमाएं नहीं हैं, जितना मैंने प्रभात को समझा है,दावा कर सकता हूं कि उन्हें अपनी सीमाओं का भरपूर अहसास है. लबों पे ये दुआ आ रही है कि आगे भी रहे. उन्होंने ही कहा है कि
बरते जाने से घिसती हैं झाड़ू की सीकें
समय की रगड़ से टूटती हैं कविताएं

इन कविताओं के द्वारा उन्होंने कविता की जमीन तोड़ी है, उम्मीद करता हूं कि अपने अगले संग्रह में इस जमीन को भी तोड़ेंगे.
___________
(राकेश बिहारी द्वरा संपादित अकार के अंक में प्रकाशित आलेख का संवर्धित रूप)
___________
(राकेश बिहारी द्वरा संपादित अकार के अंक में प्रकाशित आलेख का संवर्धित रूप)
प्रमोद कुमार तिवारी
गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय
गांधीनगर- 382030
pramodktiwari@gmail.com/मो. 09228213554